Table of Contents
परिचय
इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया और जाना कि पिछले 69 वर्षों में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना। लेकिन, क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश-शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता-आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की ज़रूरत क्यों महसूस की? उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बाँधने का फ़ैसला क्यों किया? इस पुस्तक में बार-बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है। यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों ज़रूरी है? इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरे, यह प्रश्न पूछना भी ज़रूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वह कैसा है? इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं? क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति-बोध जुड़ा हुआ है? और अगर एेसा है, तो यह नीति-बोध स्वयं में क्या है? हमारे संविधान के पीछे कौन-सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है? इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएँ क्या हैं और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमज़ोरियाँ क्या हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे।
इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि -
➤ संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों ज़रूरी हैं,
➤ भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएँ क्या हैं,
➤ इस संविधान की आलोचनाएँ क्या हैं, और
➤ इस संविधान की सीमाएँ क्या हैं।
संविधान के दर्शन का क्या आशय है?
कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिलकुल ही अलग बात, इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता किंतु बहुत-से कानून एेसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है।
इसी कारण संविधान को एक एेसे दस्तावेज़ के रूप में देखना ज़रूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नज़रिये से हमारा क्या आशय है? इसमें तीन बातें शामिल हैं –
➤ पहली बात, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों, जैसे – ‘अधिकार’, ‘नागरिकता’, ‘अल्पसंख्यक’ अथवा ‘लोकतंत्र’ के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें।
➤ इसके अतिरिक्त, हमारे सामने एक एेसे समाज और शासन-व्यवस्था की तस्वीर साफ-साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए।

क्या इसका मतलब यह माना जाए कि हर संविधान का एक दर्शन होता है या सिर्फ कुछ ही संविधानों में दर्शन होता है?
➤ इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक हैं तथा आगे उनमें कौन-से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं, तो हमारे लिए यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा।
सन् 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में ‘शांति संविधान’ कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है - ‘‘हम, जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं’’। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है –
जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है –
1. न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा-सर्वदा के लिए दूर रहेंगे।
2. उपर्युक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए ज़मीनी-सेना, नौ-सेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो-सामान कभी भी नहीं रखे जाएँगे।
इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियाँ किस तरह संविधान निर्माताओं के सोच पर छाई रहती हैं।

जी हाँ, बिलकुल! संविधान की विभिन्न व्याख्याओं की बात मुझे याद है। हमने पिछले अध्याय में इस पर चर्चा की थी। की थी न?
संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज-व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य-समूह से दिशा-निर्देशित करने का फ़ैसला किया, तो एेसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य-समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे, भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट न हों, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों न हों, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्त्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। एेसा करना इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग-अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जाँच सकें। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत-से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भाँति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया बल्कि इन पर बार-बार अदालतों में जिरह होती है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों – विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में विचार-विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग-अलग ढंग से की जाती है और कभी-कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की ज़रूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं? कभी-कभी विभिन्न संस्थाएँ एक ही आदर्श की व्याख्या अलग-अलग ढंग से करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की ज़रूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग-अलग ढंग से की जाए, तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। यह जाँचने की ज़रूरत आ पड़ती है कि कौन-सी व्याख्या सही है। इस जाँच-परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है।
संविधान–लोकतांत्रिक बदलाव का साधन
पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की ज़रूरत के बारे में पढ़ा। इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर हैं। बल प्रयोग और दंड-शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। यदि एेसे राज्य की संस्थाएँ गलत हाथों में पड़ जाएँ तो क्या होगा? भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती हैं। राज्य की शक्ति का दुनियाभर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुँचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अगर एेसा है, तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सबके अतिरिक्त, औपनिवेशिक दासता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि संविधान सभा की माँग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक माँग का प्रतिरूप है क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे, नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जन-प्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है बल्कि यह स्वयं में ‘राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढाँचे के खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है।’ भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊँच-नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नये युग में प्रवेश के लिए हुआ।

क्या हम यह कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य सामाजिक बदलाव के लिए आतुर थे? लेकिन, हम तो यह भी कहते हैं कि संविधान सभा में हर तरह के विचार रखे गए!
इस नज़रिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है। इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान, कमज़ोर लोगों को उनका वाज़िब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है।
संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें?
पीछे क्यों मुड़ें और अपने को अतीत से क्यों बाँधकर रखें? कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है? किंतु, राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों ज़रूरी है? क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन-किन बातों में सही-गलत का फ़ैसला दे सकता है?
खुद करें — खुद सीखें
अध्याय दो और सात में दिए गए संविधान सभा की बहस के उद्धरणों को एक बार फिर पढ़ें। क्या आप मानते हैं कि इन अंशों में दिए गए तर्क आज के समय में प्रासंगिक हैं? क्यों?
अमेरिका का उदाहरण लें। वहाँ संविधान 18 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लिखा गया। उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21 वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल, हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान-निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं-उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है।
हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार-बरताव के पीछे जो असली बात है, हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है, वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो, भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार-बरताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। जब तक सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता। लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार-बरताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना ज़रूरी हो जाता है। एेसे में इन व्यवहारों-बरतावोें के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। संभव है, इस क्रम में हमें और पीछे यानि औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े। इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार-बार याद करना और उससे टटोलना हमारे लिए ज़रूरी है।
हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है?
इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अँटने से इनकार करता है क्योंकि यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन-मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ-साथ एेतिहासिक रूप से अधिकार, वंचित वर्गों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्व सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्व संविधान है। संक्षेप में यह संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक न एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। इन सबके साथ एक बुनियादी चीज़ और है – संविधान का ज़ोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए।

यह कठिन है। हमें सीधे- सीधे क्यों नहीं बता दिया जाता कि इस संविधान का दर्शन क्या है? यदि यह दर्शन एेसे छुपा रहेगा तो आम नागरिक इसे कैसे समझेगा?

इस खेल के मैदान में हर विचार को दौड़ लगाने की छूट है लेकिन ‘अंपायर’ लोकतंत्र है।
व्यक्ति की स्वतंत्रता
संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द-गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन-मनन करने से नहीं आई। यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही राममोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट-छाँट का विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राममोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। इसलिए, राज्य के लिए ज़रूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश-शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की माँग निरंतर उठाते रहे। आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरह, मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आखिर कुख्यात रौलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य वैयक्तिक स्वतंत्रताएँ मसलन अंतरात्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्त्व देता है। यहाँ इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के चालीस वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। इसे यों ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था बल्कि इसे एक एेसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता।
सामाजिक न्याय
जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान योरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप ‘उदारवाद’ के बारे में और समझेंगे। शास्त्रीय उदारवाद (classical liberalism) सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायनों में अलग है। पहली बात तो यह कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की ज़रूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सका।
कहाँ पहुुँचे? क्या समझे ?
बताएँ कि निम्नलिखित में कौन-सा अधिकार वैयक्तिक स्वतंत्रता का अंश है?
➤ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
➤ धर्म की स्वतंत्रता
➤ अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
➤ सार्वजनिक स्थलों पर बराबरी की पहुँच।
विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान
संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन-मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। हमारे देश में एेसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदायों के बीच अकसर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। समुदायों के बीच एक-दूसरे के साथ अकसर ऊँच-नीच का रिश्ता होता है जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं। दूसरे, जब समुदाय एक-दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊँच-नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंद्विता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए? समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए? समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में एेसा ही किया गया है। लेकिन एेसा करना न तो अपने देश में कारगर होता और न ही वांछनीय। इसका कारण यह नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और एेसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति-रिवाज तथा भाषा होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है। उदाहरण के लिए, फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन-मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए – इस बात को सुनिश्चित करना ज़रूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना ज़रूरी हो गया।
के एम पणिक्कर – भारतीय उदारवाद की दो धाराएँ हैं। पहली धारा की शुरुआत राममोहन राय से होती है। उन्हाेंने व्यक्ति के अधिकारों पर ज़ोर दिया, खासकर महिलाओं के अधिकार पर। दूसरी धारा में स्वामी विवेकानंद, के सी सेन और जस्टिस रानाडे जैसे चिंतक शामिल हैं। इन चिंतकों ने पुरातनी हिन्दू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया। विवेकानंद के लिए हिंदू समाज की एेसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव न होता।
- इन डिफेंस अॉव लिबरलिज़्म-बॉंबे-एशिया पब्लि. हाऊस, 1962

सामाजिक न्याय की बात करते हुए हमें नीति-निर्देशक सिद्धांतों की बात भी नहीं भूलनी चाहिए।

मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन? मेरी बहुत-सी पहचान है। मेरी धार्मिक पहचान है; मेरी भाषाई पहचान है; मेरा रिश्ता अपने पैतृक शहर से है और फिर मैं एक छात्र भी हूँ।
एेसे ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार। एेसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता।
धर्मनिरपेक्षता
माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को ‘निजी मामला’ के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ यह कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? एेसी बात नहीं हैं। यद्यपि शुरुआत में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा। हाँ, यह भी है कि मुख्यधारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है।

क्या हमें राजनीतिक- सिद्धांत का पाठ्यक्रम पढ़ाने की शुरुआत हो गई है?
इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे। पारस्परिक निषेध (mutual exclusion) शब्द का अर्थ होता है – धर्म और राज्य दोनों एक-दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए ज़रूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल न दे और न ही राज्य-संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में, पारस्परिक-निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए।
धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के इस मुख्यधारा के नज़रिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे यह तक बताने लगें कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा-प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन, जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा? इसलिए, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी ज़रूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण, राज्य के लिए भी ज़रूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुँचाए। संक्षेप में, राज्य को चाहिए कि वह न तो धर्म की मदद करे और न ही उसे बाधा पहुँचाए। इसके बदले, राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना ज़रूरी है।
ठीक इसी तरह, राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार न बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बँट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था। इसी कारण एेसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती, तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज़्यादा तरजीह देता। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो।
भारत में स्थितियाँ अलग थीं और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निबटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और इसके दो अलग-अलग कारण थे।
➤ धार्मिक समूहों के अधिकार
पहली बात, जैसा कि बताया जा चुका है, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही ज़रूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। इसका कारण यह कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान का भाव सीधे-सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो, तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ, अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो, एक का दूसरे पर प्रभुत्व न हो, तो इन समुदायों के सदस्य आत्म-सम्मान और आज़ादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए, भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा-संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है।

मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिरकार, धर्म के मामलों का राज्य नियमन कर सकता है या नहीं? इसके बिना, कोई धार्मिक सुधार नहीं हो सकता।
➤ राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार
दूसरी बात, धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक-निषेध नहीं हो सकता। एेसा क्यों? एेसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्म-सम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। एेसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते। राज्य एेसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा-संस्थान को वह धन दे सकता है। इस तरह, राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुँचा सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक-निषेध नहीं बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। यह एक जटिल विचार है। इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा एेसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।
हमने अभी तक तीन केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियाँ भी कहा जा सकता है।
➤ पहली बात तो यह कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक एेसे समाज में किया गया जहाँ सामुदायिक जीवन-मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं।
➤ दूसरे, हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित ‘सकारात्मक कार्य-योजना (Affirmative action programme) के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य-योजना सन् 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग दो दशक पहले ही अपना लिया था।
➤ तीसरे, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार (Group rights) (जैसे - सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार) प्रदान किए हैं। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो चार दशक बाद बहु-संस्कृतिवाद के नाम से जानी गई।
सार्वभौम मताधिकार
दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं, खासतौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊँच-नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्त्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहाँ लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी देर से दिया गया था। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात्य तबके में जगह बना ली, तो इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक स्व-शासन का विचार भी पनपा। इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक एेसी राजव्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज–विचारों में एक है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास ‘कंस्टिट्यूशन अॉफ इंडिया बिल’ के नाम से सन् 1895 में हुआ था। इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात् भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट (1928 ई.) में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को (स्त्री हो या पुरुष) लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में एेसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भू-सीमा में पैदा हुआ है और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है अथवा जिसके पिता इस भू-सीमा में जन्म हों या बस गए हों। इस तरह, शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्त्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इज़हार करती है।
सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए तथा इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत, सबका भला करेगी।
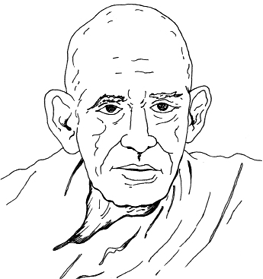
अलादि कृष्णस्वामी अय्यर
संविधान सभा के वाद-विवाद, खंड XI, पृष्ठ 835, 23 नवंबर 1949

सचमुच यह गर्व की बात है कि ‘एक व्यक्ति - एक वोट’ का सिद्धांत लगभग बगैर किसी ना-नुकर के मान लिया गया। क्या यह बात सच नहीं कि बहुत से देशों में मताधिकार के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा।
संघवाद
जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने ‘असमतोल संघवाद’ जैसी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्त्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहें अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाय।
मसलन, भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। यह एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 ये के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नगालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद न सिर्फ नगालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी एेसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बरताव में कोई बुराई नहीं है।

मैं सचमुच चकित हूँ। कौन कहता है कि हमारा संविधान सिर्फ नकल है। हर ‘बाहरी’ अंश पर हमने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है।
हालाँकि संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई है परंतु आज भारत एक बहु-भाषिक संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा-पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है।
राष्ट्रीय पहचान
संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर ज़ोर दिया गया है। इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करें। ऊपर की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग-अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन-मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया। संविधान में एेसे निर्वाचन-मंडल की बात नकार दी गई। पृथक निर्वाचन-मंडल की बात को नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय-जीवन सहजता में बाधा पहुँचती है।
प्रक्रियागत उपलब्धि
ऊपर बताई गई पाँच केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियाँ प्रक्रियागत भी हैं।
➤ अव्वल तो यह कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार-विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत-से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी। लेकिन, इस सभा की बहसों से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नज़रिया यथा संभव सबको शामिल करने का था। यह खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं बल्कि तर्कबुद्धि की तुला पर तौलकर परखने के लिए तैयार है। इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे।
लेकिन आगे चलकर यह भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज़ है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है...
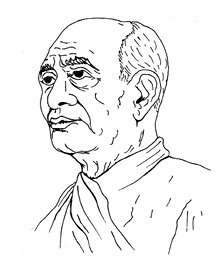
सरदार पटेल
संविधान सभा के वाद-विवाद, खंड VIII, पृष्ठ 272, 25 मई 1949
➤ दूसरे, इससे सुलह और समझौते के जज़्बे का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज़ का सौदा कर लिया जाता है, तो यह समझौता बुरा है। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है, तो एेसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए परंतु है नहीं। फिर भी, हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर फ़ैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाय। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है।
आलोचना
भारतीय संविधान की कई आलोचनाएँ हैं। इनमें से तीन पर यहाँ संक्षेप में चर्चा की जाएगी- (क) यह संविधान अस्त-व्यस्त है। (ख) इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है।
(ग) यह संविधान भारतीय परिस्थितियों केअनुकूल नहीं है।
भारतीय संविधान को अस्त-व्यस्त या ढीला-ढाला बताया जाता है। इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज़ के रूप में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है जहाँ संविधान एक कसे हुए दस्तावेज़ के रूप में है। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज़ तो होता ही है इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेज़ों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह, इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्त्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज़ से बाहर मिलें जिसे ‘संविधान’ कहा जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है - संविधान हैसियत के एेसे बहुत-से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज़ के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर, बहुत-से देशों के संवैधानिक दस्तावेज़ में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में एेसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं।

संस्थाओं की बनावट में समझौते की बात तो समझ में आती है लेकिन परस्पर विरोधी सिद्धांतों को एक में कैसे समेटा जा सकता है?
क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके के थे। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी?
यहाँ ज़रूरी है कि हम नुमाइंदगी के दो हिस्सों में फर्क करें। इसमें एक को हम चाहें तो ‘आवाज़’ कह सकते हैं और दूसरे को ‘राय’। नुमाइंदगी में ‘आवाज़’ अपने आप में महत्त्वपूर्ण हैं। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज़ से होनी चाहिए न कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज़ से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर-नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे न कि सार्वभौम मताधिकार से। बहरहाल, अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी ‘राय’ पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर-नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट ज़रूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत-से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए।
क्या यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है। यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इज़हार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है।
एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज़ है। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत-से सदस्यों ने यह बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गति-मति भारत की असली जनता और उसके आचार-विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गति-मति के अनुकूल नहीं है।
यह आरोप कितना सच है?
यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है। लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता? पहली बात तो यह कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया है बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राम मोहन राय से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी और आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन् 1841 में ही यह बात जाहिर हो गई थी। उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले ‘दलित’ नए कानूनों का इस्तेमाल करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

बिलकुल! क्या पहले अध्याय में हमने यही बात नहीं सीखी कि समाज के हर तबके के पास संविधान को मानने का कोई वैध कारण होना चाहिए?
दूसरे, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर-संस्कृति उत्पन्न हुई। यह संकर-संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी एेसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूँढा जा सकता है और न ही देशी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देशी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर-पश्चिमी मुल्कों में, लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह, जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है न कि नकल का।
...हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। एेसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे।... यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक न था।
के. हनुमन्थैया
संविधान सभा के वाद-विवाद, खंड XI, पृष्ठ 616-617, 17 नवंबर 1949
सीमाएंँ
इन बातों का यह मतलब नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज़ है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएँ - एेसी बातें बच जाएँ जिनके पुनरावलोकन की ज़रूरत हो। इस संविधान की बहुत-सी एेसी बातें समय के दबाव में पैदा हुईं। फिर भी, हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएँ हैं।
अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं की चर्चा कर लें।
पहली बात यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरे, इसमें लिंगगत-न्याय के कुछ महत्त्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है।
तीसरे, यह बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया?
संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है। लेकिन यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क यह है कि संविधान की ये सीमाएँ इतनी गंभीर नहीं हैं कि ये संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर दें।
निष्कर्ष
इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है। संविधान की केंद्रीय विशेषताएँ उसे जीवंत बनाती हैं। कानूनी प्रावधान और संस्थानिक-व्यवस्था समाज की ज़रूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर हैं। इस पुस्तक में हमने जिस संस्थानिक-व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके मूल में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि। इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है। यह दृष्टि एेतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान किया। इस तरह संविधान में यह दृष्टि रूपायित हुई। बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार-संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है।
क्या आपने ध्यानपूर्वक संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है? इसमें बहुत से उद्देश्यों का जिक्र तो है ही, साथ में एक विनम्र दावेदारी भी है। इस संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया। इसकी रचना और इसका अंगीकार ‘हम भारत के लोग’ के द्वारा हुआ। इस तरह जनता स्वयं अपनी नियति की नियंता है और लोकतंत्र एक साधन है जिसके सहारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। आज प्रस्तावना के इस उद्घोष को पचास साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं। हमने देखा है कि अदालतों और सरकारों के बीच अनेक व्याख्याओं पर असहमति है। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मत-वैभिन्न है। राजनीतिक दल संविधान की विविध व्याख्याओं के आधार पर पूरे ज़ोर-शोर से लड़ते हैं। अगले साल आप पढ़ेंगे कि हमारी राजनीति में बहुत सी समस्याएँ और कमियाँ हैं। फिर भी, अगर आप किसी राजनेता अथवा आम नागरिक से पूछें तो पाएँगे कि हर कोई संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है। हम सब साथ रहना चाहते हैं और समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता की भावना के आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं। संविधान की दृष्टि अथवा दर्शन में यह साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्त्वपूर्ण परिणाम है। सन् 1950 में इस संविधान का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। आज, इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

कोई भी दस्तावेज़ पूर्ण नहीं हो सकता और कोई भी आदर्श पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन, क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम कोई आदर्श अपनाएँ ही नहीं? भविष्य का कोई सपना पालें ही नहीं? क्या मैं सही कह रही हूँ?
प्रश्नावली
1. नीचे कुछ कानून दिए गए हैं। क्या इनका संबंध किसी मूल्य से है? यदि हाँ, तो वह अंतर्निहित मूल्य क्या है? कारण बताएँ।
(क) पुत्र और पुत्री दोनों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा होगा।
(ख) अलग-अलग उपभोक्ता वस्तुओें के बिक्री-कर का सीमांकन अलग-अलग होगा।
(ग) किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
(घ) ‘बेगार’ अथवा बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती।
2. नीचे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं। बताएँ कि इसमें किसका इस्तेमाल निम्नलिखित कथन को पूरा करने में नहीं किया जा सकता?
लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत...
(क) सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है।
(ख) अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए होती है।
(ग) औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है।
(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्षणिक आवेग में दूरगामी के लक्ष्यों से कहीं विचलित न हो जाएँ।
(ङ) शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए होती है।
3. संविधान सभा की बहसों को पढ़ने और समझने के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं – (अ) इनमें से कौन-सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान सभा की बहसें आज भी प्रासंगिक हैं? कौन-सा कथन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि ये बहसें प्रासंगिक नहीं हैं। (ब) इनमें से किस पक्ष का आप समर्थन करेंगे और क्यों?
(क) आम जनता अपनी जीविका कमाने और जीवन की विभिन्न परेशानियों के निपटारे में व्यस्त होती हैं। आम जनता इन बहसों की कानूनी भाषा को नहीं समझ सकती।
(ख) आज की स्थितियाँ और चुनौतियाँ संविधान बनाने के वक्त की चुनौतियों और स्थितियों से अलग हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को पढ़ना और अपने नए जमाने में इस्तेमाल करना दरअसल अतीत को वर्तमान में खींच लाना है।
(ग) संसार और मौजूदा चुनौतियों को समझने की हमारी दृष्टि पूर्णतया नहीं बदली है। संविधान सभा की बहसों से हमें यह समझने के तर्क मिल सकते हैं कि कुछ संवैधानिक व्यवहार क्यों महत्त्वपूर्ण हैं। एक एेसे समय में जब संवैधानिक व्यवहारों को चुनौती दी जा रही है, इन तर्कों को न जानना संवैधानिक-व्यवहारों को नष्ट कर सकता है।
4. निम्नलिखित प्रसंगों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर स्पष्ट करें –
(क) धर्मनिरपेक्षता की समझ
(ख) अनुच्छेद 370 और 371
(ग) सकारात्मक कार्य-योजना या अफरमेटिव एक्शन
(घ) सार्वभौम वयस्क मताधिकार
5. निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन-सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है?
(क) राज्य का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।
(ख) राज्य का धर्म से नजदीकी रिश्ता है।
(ग) राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है।
(घ) राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार को मान्यता देगा।
(ङ) राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्ति होगी।
6. निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करें –
(क) विधवाओं के साथ किए जाने वाले- आधारभूत महत्व की उपलब्धि
बरताव की आलोचना की आज़ादी।
(ख) संविधान सभा में फ़ैसलों का स्वार्थ- प्रक्रियागत उपलब्धि
के आधार पर नहीं बल्कि तर्कबुद्धि
के आधार पर लिया जाना।
(ग) व्यक्ति के जीवन में समुदाय के लैंगिक-न्याय की उपेक्षा
महत्त्व को स्वीकार करना।
(घ) अनुच्छेद 370 और 371 उदारवादी व्यक्तिवाद
(ङ) महिलाओं और बच्चों को परिवार धर्म-विशेष की ज़रूरतों के प्रति
की संपत्ति में असमान अधिकार। ध्यान देना
7. यह चर्चा एक कक्षा में चल रही थी। विभिन्न तर्कों को पढ़ें और बताएँ कि आप इनमें किस-से सहमत हैं और क्यों?
जयेश– मैं अब भी मानता हूँ कि हमारा संविधान एक उधार का दस्तावेज़ है।
सबा – क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इसमें भारतीय कहने जैसा कुछ है ही नहीं? क्या मूल्यों और विचारोें पर हम ‘भारतीय’ अथवा ‘पश्चिमी’ जैसा लेबल चिपका सकते हैं? महिलाओं और पुरुषों की समानता का ही मामला लो। इसमें ‘पश्चिमी’ कहने जैसा क्या है? और, अगर एेसा है भी तो क्या हम इसे महज पश्चिमी होने के कारण खारिज कर दें?
जयेश– मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद क्या हमने उनकी संसदीय-शासन की व्यवस्था नहीं अपनाई?
नेहा – तुम यह भूल जाते हो कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ़ थे। अब इस बात का, शासन की जो व्यवस्था हम चाहते थे उसको अपनाने से कोई लेना-देना नहीं, चाहे यह जहाँ से भी आई हो।
8. एेसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधिमूलक नहीं थी? क्या इस कारण हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं रह जाता? अपने उत्तर के कारण बताएँ।
9. भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक-न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन-से प्रमाण देंगे। यदि आज आप संविधान लिख रहे होते, तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में किन प्रावधानों की सिफारिश करते?
10. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि – ‘एक गरीब और विकासशील देश में कुछ एक बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकारों की केंद्रीय विशेषता के रूप में दर्ज करने के बजाए राज्य की नीति-निर्देशक तत्त्वों वाले खंड में क्यों रख दिए गए – यह स्पष्ट नहीं है।’ आपके जानते सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को नीति-निर्देशक तत्त्व वाले खंड में रखने के क्या कारण रहे होंगे?
11. आपके विद्यालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाया?
अपनी राय ज़रूर दें –
आपको यह किताब कैसी लगी? इसे पढ़ने या इसका प्रयोग करने का आपका अनुभव कैसा रहा? आपको इसमें क्या-क्या परेशानियाँ हुईं? पुस्तक के अगले संस्करण में आप इसमें क्या-क्या बदलाव चाहेंगे? इन सबके बारे में या किसी भी नए सुझाव के संबंध में हमें अवश्य लिखें। आप अध्यापक हों, अभिभावक हों, छात्र हों या सामान्य पाठक, हर कोई सलाह दे सकता है। किताबों में बदलाव की प्रक्रिया में आपके सुझाव अमूल्य हैं। हम हर सुझाव का सम्मान करते हैं।
कृपया हमें इस पते पर लिखेंः
समन्वयक (राजनीति विज्ञान)
सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016
