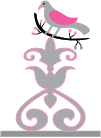Table of Contents

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर
 18
18
जन्मः 14 अप्रैल, सन् 1891, महू (मध्य प्रदेश)में
प्रमुख रचनाएँः दॅकास्ट्स इन इंडिया, देयर मेकेनिज़्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट (1917, प्रथम प्रकाशित कृति);
द अनटचेबल्स, हू आर दे? (1948); हू आर द शूद्राज़ (1946); बुद्धा एंड हिज़ धम्मा (1957); थाट्स अॉन लिंग्युस्टिक स्टेट्स (1955); द प्रॉब्लम अॉफ़ द रुपी(1923);
द एबोलुशन अॉफ़ प्रोविंशियल फ़ायनांस इन ब्रिटिश इंडिया (पीएच.डी. की थीसिस, 1916); द राइज़ एंडफ़ॉल अॉफ़ द हिंदू वीमैन (1965); एनीहिलेशन अॉफ़ कास्ट(1936); लेबर एंड पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी(1943); बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज़्म(1956), (पुस्तकें व भाषण); मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता(पत्रिका-संपादन); हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अांबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है
निधनः दिसंबर, सन् 1956 दिल्ली में
अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस
सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है।
मानव-मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयार्क(अमेरिका)फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के ज़रिये पढ़ा और एेतिहासिक-सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत कीं। सब मिलाकर वे इतिहास-मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद् तथा धर्म-दर्शन के व्याख्याता बन कर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मज़दूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया।
भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉ. भीमराव अांबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉ. अांबेडकर को बचपन से ही जाति-आधारित उत्पीड़न-शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि "तुम पढ़-लिख कर क्या बनोगे?" तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था मैं पढ़-लिख कर वकील बनूँगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊँगा और छुआछूत को खत्म करूँगा। डॉ. अांबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन-मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नयी अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दासता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दासता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी।
उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे–बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्तूबर, सन् 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए।
भारत के संविधान-निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वत्ता एकांत ज्ञान-साधना की जगह मानव-मुक्ति व जन-कल्याण के लिए थी–यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए।
यहाँ प्रस्तुत पाठ आंबेडकर के विख्यात भाषण एनीहिलेशन अॉफ़ कास्ट (1936) के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी-रूपांतर जाति-भेद का उच्छेद के दो प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति-पाँति तोड़क मंडल (लाहौर) के वार्षिक सम्मेलन (सन् 1936) के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था; परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में, आंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता– ये तीन तत्त्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति-मज़हब आधारित विषाक्त सामाजिक-राजनैतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है।
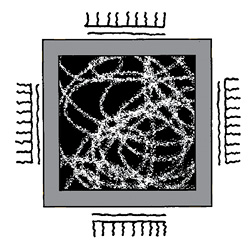
श्रम विभाजन और जाति-प्रथा
यह विडंबना की ही बात है, कि इस युग में भी ‘जातिवाद’ के पोषकों की कमी नहीं हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, कि आधुनिक सभ्य समाज ‘कार्य-कुशलता’ के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूँकि जाति-प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, कि जाति-प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक-विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति-प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे की अपेक्षा ऊँच-नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता।
जाति-प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम-श्रमिक-समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति-प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता-पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है।
जाति-प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्वनिर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन-भर के लिए एक पेशे में बाँध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग-धंधों की
प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को एेसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति-प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति-प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति-प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्त्व नहीं रहता। ‘पूर्व लेख’ ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग ‘निर्धारित’ कार्य को ‘अरुचि’ के साथ केवल विवशतावश करते हैं। एेसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। एेसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति-प्रथा हानिकारक प्रथा है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणारुचि व आत्म-शक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है।
मेरी कल्पना का आदर्श-समाज
जाति-प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते-सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति-प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श-समाज क्या है? ठीक है, यदि एेसा पूछेंगे, तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श-समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है, भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श-समाज में इतनी गातिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। एेसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध-पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो।
इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई ‘स्वतंत्रता’ का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औज़ार व सामग्री रखने के अधिकार जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी ‘स्वतंत्रता’ पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए?
जाति-प्रथा के पोषक, जीवन, शारीरिक-सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे ‘दासता’ में जकड़कर रखना होगा, क्योंकि ‘दासता’ केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। ‘दासता’ में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह एेसे वर्ग होना संभव है, जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं।
अब आइए समता पर विचार करें। क्या ‘समता’ पर किसी की आपत्ति हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में ‘समता’ शब्द ही विवाद का विषय रहा है। ‘समता’ के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। और उनका यह तर्क वज़न भी रखता है। लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्त्व नहीं रखता। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में ‘समता’ असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता तीन बातों पर निर्भर रहती है। (1) शारीरिक वंश परंपरा, (2) सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता-पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि, सभी उपलब्धियाँ जिनके कारण सभ्य समाज, जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, और अंत में (3) मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण, समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है?
व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से, असमान प्रयत्न के कारण, असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित हैं? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाज़ी मार ले जाएँगे, जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही ‘उत्तम व्यवहार’ का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाज़ा यह है कि जहाँ हम तीसरे (प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है) आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम दो आधारों (जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं) पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। और हमें एेसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो यह तो संभव है, जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए।
‘समता’ का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता। इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय, राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अलग-अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग-अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, ‘मानवता’ के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बाँटा जा सकता। एेसी स्थिति में, राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है, कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता।
इस प्रकार ‘समता’ यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है।
अभ्यास
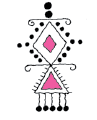

पाठ के साथ
1. जाति प्रथा को श्रम-विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अांबेडकर के क्या तर्क हैं?
2. जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है?
3. लेखक के मत से ‘दासता’ की व्यापक परिभाषा क्या है?
4. शारीरिक वंश-परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद आंबेडकर ‘समता’ को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं?
5. सही में आंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन-सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं?
6. आदर्श समाज के तीन तत्त्वों में से एक ‘भ्रातृता’ को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस ‘भ्रातृता’ शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे/समझेंगी?

पाठ के आसपास
1. आंबेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन न होने की जो बात की है–उस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी ‘गलता लोहा’ पर पुनर्विचार कीजिए।
2. कार्य कुशलता पर जाति प्रथा का प्रभाव विषय पर समूह में चर्चा कीजिए। चर्चा के दौरान उभरने वाले बिंदुओं को लिपिबद्ध कीजिए।

इन्हें भी जानें
* आंबेडकर की पुस्तक जातिभेद का उच्छेद और इस विषय में गांधी जी के साथ उनके संवाद की जानकारी प्राप्त कीजिए।
* हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने कैसे आदर्श समाज की कल्पना की है, उसे भी पढ़ें।