Table of Contents

ब्रजमोहन व्यास
(सन् 1886-1963)
ब्रजमोहन व्यास का जन्म इलाहाबाद में हुआ। पं. गंगानाथ झा और पं. बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी सन् 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगरपालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। सन् 1944 से 1951 के लीडर समाचारपत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं–जानकी हरण (कुमारदास कृत) का अनुवाद, पं. बालकृष्ण भट्ट (जीवनी), महामना मदन मोहन मालवीय (जीवनी)। मेरा कच्चा चिट्ठा उनकी आत्मकथा है।
व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है जिसमें दो हज़ार पाषाण मूर्तियाँ, पाँच-छह हज़ार मृणमूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएँ, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी-फ़ारसी के चौदह हज़ार हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पं. नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है।
पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर-सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम-कौशल और मेधा कार्य का ‘कच्चा चिट्ठा’ है।


कच्चा चिट्ठा

सन् 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्वक्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहाँ का काम निबटाकर सोचा कि दिनभर के लिए पसोवा हो आऊँ। ढाई मील तो हई है। सौभाग्य से गाँव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। उस इक्के को ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया। कील-काँटे से दुरस्त था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर-दूर से हज़ारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी-सी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था।
यह भी किंवदंती है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। पसोवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिह्न अब शेष नहीं रह गए, परंतु वहाँ एक पहाड़ी अवश्य है। ‘निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिं दृढ़यति’–(भवभूति)। पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है।
मैं कहीं जाता हूँ तो छूँछे हाथ नहीं लौटता। यहाँ कोई विशेष महत्त्व की चीज़ तो नहीं मिली पर गाँव के भीतर कुछ बढ़िया मृण्मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिल गए। इक्के पर कौशाम्बी लौटा। एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे-से गाँव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच, पेड़ के नीचे, एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अब आप ही बताइए, मैं करता ही क्या? यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। इक्के से उतरकर इधर-उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वज़न में रही होगी। ‘न कूकुर भूँका, न पहरू जागा।’ मूर्ति अच्छी थी। पसोवे से थोड़ी सी चीज़ों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। उसे लाकर नगरपालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया।
उसके थोड़े ही दिन बाद गाँववालों को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव वहाँ से अंतर्धान हो गए। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मानसिंह अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गाँववालों का संदेह मुझपर होता था। और कैसे न हो? ‘अपना सोना खोटा तो परखवैया का कौन दोस?’ मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि 95 प्रतिशत उनका संदेह सही निकलता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ़्तर में बैठा काम कर रहा था।
चपरासी ने आकर इत्तिला की कि पसोवे के निकटस्थ एक गाँव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा माथा ठनका। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया। उसमें बुड्ढ़े, जवान, स्त्रियाँ, बच्चे सभी थे। संभव है, धर्म पर आघात समझकर आसपास के गाँव के भी कुछ लोग साथ में चले आए हों।
मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, "महाराज! (मेरे मस्तक पर हस्बमामूल चंदन था) जब से शंकर भगवान हम लोगन क छोड़ के हियाँ चले आए, गाँव भर पानी नै पिहिस। अउर तब तक न पी जब तक भगवान गाँव न चलिहैं। अब हम लोगन क प्रान आपै के हाथ में हैं। आप हुकुम देओ तो हम भगवान को लेवाए जाइ।" यदि मुझे मालूम होता कि गाँववालों को उन पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी न लाता। मैंने तुरंत कहा, "आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएँ।" सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैंने स्वयं शेड पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। स्त्री-पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना आरंभ कर दिया। मैंने मिठाई और जल मँगाकर उन लोगों का उपवास तुड़वाया। दूर से दफ़्तर वाले अपने अफ़सर की करतूत देखकर मुसकरा रहे थे। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके दो-तीन आदमियों को साथ लेकर लारी के अड्डे पर पहुँचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा किया। गाँववालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का भी तो खयाल था।
यह रवैया मेरा बराबर जारी रहा। उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष, मैं फिर कौशाम्बी गया और गाँव-गाँव, नाले-खोले घूमता-फिरता झख मारता रहा। भला यह कितने दिन एेसे चल सकता, अगर बीच-बीच में छठे-छमासे कोई चीज़ इतनी महत्त्वपूर्ण न मिल जाती जिससे दिल फड़क उठता? बराबर यही सोचता कि "ना जाने केहि भेष में नारायण मिल जाएँ।" और यही एक दिन हुआ। खेतों की डाँड़-डाँड़ जा रहा था कि एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की आठ फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी। सिवाए सिर के पदस्थल तक वह संपूर्ण थी। मैं लौटकर पाँच-छह आदमी और लटकाने का सामान गाँव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा वैसे ही एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी, तमककर आई और कहने लगी, "बड़े चले हैं मूरत उठावै। ई हमार है। हम न देबै। दुइ दिन हमार हर रुका रहा तब हम इनका निकरवावा है। ई नकसान कउन भरी?" मैं समझ गया। बात यह है कि मैं उस समय भले आदमी की तरह कुरता धोती में था। इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुँह लगना ठीक नहीं। संस्कृत-साहित्य का वचन याद आया–
उद्वेजयति दरिद्रं परमुद्रायाः झणत्कारम्।
दूसरे की मुद्रा की झनझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है। उसी का आश्रय लिया। मैंने अपने जेब में पड़े हुए रुपयों को ठनठनाया। मैं एेसी जगहों में नोट-वोट लेकर नहीं जाता। केवल ठनठनाता। उसकी बात ही और होती है। मैंने कहा, "ठीकै तो कहत हौ बुढ़िया। ई दुई रुपया लेओ। तुम्हार नुकसानौ पूर होए जाई! ई हियाँ पड़े अंडसै करिहैं। न डेहरी लायक न बँडेरी लायक।" बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली, "भइया! हम मने नाहीं करित। तुम लै जाव।"
आज दिन वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगरपालिका के दफ़्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। मैंने बड़े उत्साह से उसे संपूर्ण संग्रहालय दिखलाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का एक बड़ा डीलर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीज़ें खरीदता फिरता है। मैं पहिले कैसे समझ पाता।
कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। दोनों में भेद ही क्या है। परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला, "बहुत कीमती संग्रह!" मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है। रुपयों में बतावें तो समझ में आवे। हँसकर बोला, "रुपयों में बता दूँ तो आपका ईमान डिग जाए।" वैसे ही हँसकर मैंने जवाब दिया कि "ईमान! एेसी कोई चीज़ मेरे पास हई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा-कौड़ी के हो ही नहीं सकता।"
उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा, "आप उस मूर्ति को मेरे हाथ दस हज़ार रुपए में बेचेंगे? इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियाँ मिल जाएँगी।" इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था। अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत में कहा, "यह एक ही रही।" फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकृति से मेरा निर्णय समझ लिया। बात खत्म हो गई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊँचा कर रही है।
पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा था जो दो रुपए में मिली और दस हज़ार रुपए उसपर न्योछावर कर फेंके जा रहे हैं। संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं है, (परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पग आगे बेसिर पैर की हैं। पर बात एेसी नहीं है।) यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। एेसा लेख उस मूर्ति के पदस्थल पर उत्कीर्ण है। इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया और नए सिरे से फिर मुँह में खून लग गया। शेर तो रोज़ मिलता नहीं पर चीतल, साँभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। शेर की केवल आशा मात्र रहती है। परंतु इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है और शिकारी जंगल-जंगल की खाक छानता फिरता है।
सन् 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट अॉफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के. एन. दीक्षित डायरेक्टर-जनरल थे। मेरे परम मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। साधु प्रकृति तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे, रोब था, ज़माने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से चार-पाँच मील दूर एक गाँव हजियापुर है। वहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमथ का एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे।
गाँव के एक ज़मींदार गुलज़ार मियाँ ने, जिनका गाँव में दबादबा था, एतराज़ किया। गुलज़ार मियाँ हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था, यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। मैंने उनके भाई दिलदार मियाँ को म्युनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गाँवों से पाषाण-मूर्तियाँ, शिलालेख इत्यादि देते रहते थे। मजूमदार साहब ने जब उसे ज़बरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फ़ौजदारी पर आमादा हो गए। बोले, "यह इलाहाबाद के अजायबघर के हाथ 25 रुपए का बिक चुका है, अगर बिना व्यास जी के पूछे इसे कोई उठावेगा तो उसका हाथ-पैर तोड़ देंगे।" मजूमदार साहब ने पच्छिम सरीरा के थाने में रपट की पर किसी की कुछ नहीं चली। गुलज़ार मियाँ ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इस सबकी रिपोर्ट नोन-मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिख भेजी। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था, उसने करवट ली।
एक दिन दीक्षित साहब का अर्धसरकारी पत्र मुझे मिला जिसका आशय यह था, "कौशाम्बी से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण ज़मींदार गुलज़ार मियाँ भद्रमथ के एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है और आमादा फ़ौजदारी है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता परंतु यह कहे बिना रह भी नहीं सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित है।" खैर, यहाँ तक तो खून का घूँट किसी तरह पिया जा सकता था पर इसके आगे उन्होंने लिखा, "यदि यही आपका रवैया रहा तो यह विभाग आपके कामों में वह सहानुभूति न रखेगा जो उसने अब तक बराबर रखी है।"
एक मित्र से एेसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई। मैं सबकुछ सहन कर सकता हूँ पर किसी की भी अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है। वरुणास्त्र से पानी-पानी हो जाता हूँ। मैंने तुरंत दीक्षित जी को उत्तर दिया, जो थोड़े में इस प्रकार था, "मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है, वह नितांत असत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे या न रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्रमथ के शिलालेख को 25 रुपए का खरीदा है। पर आपके विभाग से, विशेषकर आपके होते हुए, झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपए देकर ले लें, मैं गुलज़ार को लिख दूँगा।" इसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र आया जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पत्र के लिए खेद प्रगट किया। विभाग की उपेक्षा जो मैंने की थी, उसे पी गए। बात खत्म हो गई।
बाद में गुलज़ार ने मुझे बताया कि 25 रुपए लेकर उसने शिलालेख दे दिया। प्रयाग संग्रहालय में और भी भद्रमथ के शिलालेख थे, कोई क्षति नहीं हुई। गरीब ज़मींदार को 25 रुपए मिल गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि जिस गाँव में भद्रमथ का शिलालेख हो सकता है वहाँ संभव है और भी शिलालेख हों। अतः मैं हजियापुर, जो कौशाम्बी से केवल चार-पाँच मील था, गया और मैंने गुलज़ार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उसके भाई को, जो म्युनिसिपैलिटी में नौकर था, साथ ले लिया था। गुलज़ार मियाँ के मकान के ठीक सामने उन्हीं का एक निहाय
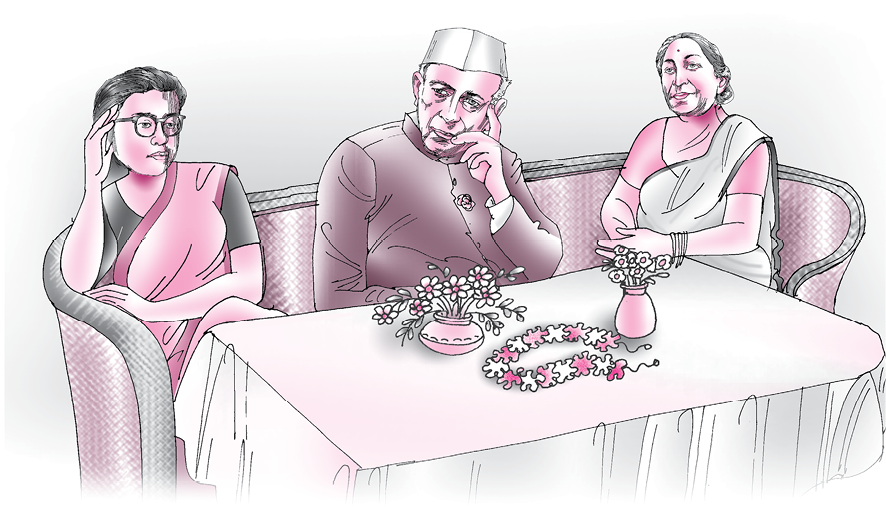
पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। आठ बड़े-बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना, चीज़ों का विस्तार। संग्रहालय के पृथक विशाल भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया। परंतु उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। यह म्याऊँ का ठौर था। सहसा एक बात सूझ गई। इस हथकंडे की दाद चाहूंँगा। ‘म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट’ में एक धारा है कि एकज़ेकेटिव आफ़िसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हरजाना (तवाना) लेकर समझौता कर ले। दूसरे, नगर में भवन-निर्माण की अनुमति देने में म्युनिसिपैलिटी ही नियमित शुल्क भी लेती थी। इन दोनों मदों से बीस हज़ार रुपया साल आय होती थी। हमने बोर्ड एवं संयुक्त प्रांत की सरकार से यह स्वीकृति ले ली कि इस आय का ‘संग्रहालय निर्माण कोष’ बना दिया जाए। इस प्रकार इस कोष में दस वर्ष के भीतर दो लाख रुपए एकत्र हो गए, जैसे–
डॉ. पन्नालाल आई.सी.एस. जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे, के सौजन्य और सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन के लिए मिल गया।
अब केवल शिलान्यास और भवन-निर्माण की देर रह गई। मैंने सोच रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से शिलान्यास कराऊँगा। उनकी-मेरी आपसदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति निष्ठा के कारण उचित ही था। मैं सिर्फ़ मौके की ताक मेें था। वह मौका आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल जी ने कहा, "व्यास! तुम्हारे म्युज़ियम की इमारत न बनेगी?"
पर मैंने नम्रता से मुसकुराते हुए उत्तर दिया, "यह मेरा अहद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास न करेंगे, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में बनने न दूँगा। पर मैं आपसे कैसे कहूँ? क्या सिवाए शिलान्यास करने के आपको और कोई काम नहीं है?" जवाहरलाल जी तुरंत बोल उठे, "यह सब फ़िजूल बात है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो शिला रख दूँगा। अब ज़्यादा देर मत करो।" बात खत्म हो गई।
उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात पर मुसकुरा रहे थे। यह तो कुछ एेसा हो गया, जैसे–लभते वा प्रार्थयिता न वा श्रियम् श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्।
–भवभूति
लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या न मिले परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है?
दो ही तीन दिन बाद डॉ. ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित कर चले गए।
निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह के साथ जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर हुआ कि "न भूतो न भविष्यति।’ परंतु उल्लेखनीय होते हुए भी उसका वर्णन न करूँगा, कारण वह कच्चे चिट्ठे की परिधि के बाहर है।
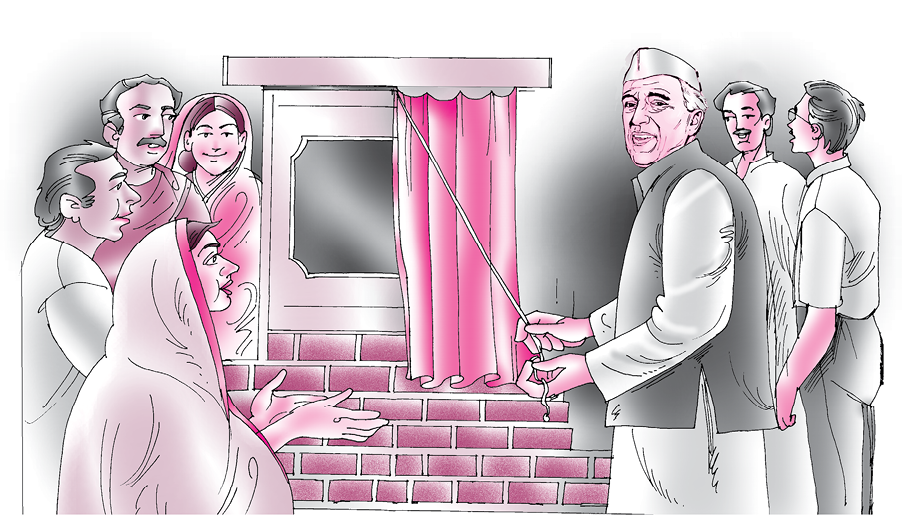
पंडित जवाहरलाल जी ने बंबई के विख्यात इंजीनियर ‘मास्टर साठे और मूता’ को लिखकर उनसे नए भवन का नक्शा बनवा दिया और समय से भवन बनकर तैयार हो गया। इस बात का मुझे संतोष है कि जनता के जिस हरजाने के रुपए से इस भवन का निर्माण हुआ उसे मैंने पाई-पाई ब्याज सहित (संगृहीत चीज़ें पंद्रह लाख से कम की नहीं हैं) उन्हें ‘प्रजानामेव भूत्यर्थम्’ लौटा दिया।
एक बात और। इसके पहिले कि मैं इस ‘कच्चे चिट्ठे’ को समाप्त करूँ, मैं उन लोगों से क्षमा माँगता हूँ जिन्हें मैंने छला है और फिर सिवाय मेरे क्षमा माँगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है। अपने पापों का (यदि आप उन्हें पाप समझें, मैं नहीं समझता) प्रायश्चित तो मैंने लिखकर कर लिया। परंतु समाप्त करते-करते मैं एेसी कृतघ्नता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। यह संग्रहालय चार महानुभावों के साहाय्य और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ (तत्कालीन चेयरमैन), हिज़ हाइनेस
श्री महेंद्रसिंहजू देव नागौद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्रसिंह जिनके भरहुत और भुमरा संग्रह के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊँचा है और मेरा स्वामीभक्त अर्दली जगदेव, जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ। ठाकुर ने ठीक ही कहा है–
सामिल मैं पीर मैं सरीर मैं न राखै भेद
हिम्मत कपाट को उघारै तो उघरि जाय।
एेसी ठान ठानै तो बिनाहू जंत्र-मंत्र किये
साँप के जहर को उतारै तो उतरि जाय।
ठाकुर कहत कुछ कठिन न जानौ आज
हिम्मत किये ते कहौ कहा न सुधरि जाय।
चारि जने चारिहू दिसा तें चारों कोन गहि
मेरु को हिलाय के उखारैं तो उखरि जाय।।
मैं तो केवल निमित्तमात्र था। अरुण के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन-पालन किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह-प्रवेश करा दिया, उसके संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए एक सुयोग्य अभिभावक डॉ. सतीशचंद्र काला को नियुक्त कर दिया और फिर मैंने संन्यास ले लिया।
–‘मेरा कच्चा चिट्ठा’ आत्म-कथा का अंश
प्रश्न-अभ्यास
1. पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था?
2. "मैं कहीं जाता हूँ तो ‘छूँछे’ हाथ नहीं लौटता।" से क्या तात्पर्य है? लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या-क्या लाया?
3. "चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है।"–लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा और क्यों?
4. "अपना सोना खोटा तो परखवैया का कौन दोस?" से लेखक का क्या तात्पर्य है?
5. गाँववालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा? दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए।
6. लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की आठ फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ?
7. "ईमान! एेसी कोई चीज़ मेरे पास हुई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा-कौड़ी के हो ही नहीं सकता।"– के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है?
8. दो रुपए में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर दस हज़ार रुपए क्यों न्यौछावर किए जा रहे थे?
9. भद्रमथ शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई? स्पष्ट कीजिए।
10. लेखक अपने संग्रहालय के निर्माण में किन-किन के प्रति अपना आभार प्रकट करता है और किसे अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निशि्ंचत होता है?
भाषा शिल्प
1. निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए–
(क) इक्के को ठीक कर लिया
(ख) कील-काँटे से दुरूस्त था।
(ग) मेरे मस्तक पर हस्बमामूल चंदन था
(घ) सुरखाब का पर
2. लोकोक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए-
(क) चोर की दाढ़ी में तिनका
(ख) ना जाने केहि भेष में नारायण मिल जाएँ
(ग) यह म्याऊँ का ठौर था
योग्यता-विस्तार
1. अगर आपने किसी संग्रहालय को देखा हो तो पाठ से उसकी तुलना कीजिए।
2. अपने नगर में अथवा किसी सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय को देखने की योजना बनाएँ।
3. लोकहित संपन्न किसी बड़े काम को करने में ईमान / ईमानदारी आड़े आए तो आप क्या करेंगे।
शब्दार्थ और टिप्पणी
किंवदंती - लोगों द्वारा कही गई
सन्निकट - पास, नज़दीक
छूँछे - बुद्धू (बनना, बनाना) खाली
अंतरधान - छिप जाना, गायब हो जाना
प्रख्यात - बहुत प्रसिद्ध
इत्तिला - सूचना, खबर
उत्कीर्ण - खुदा हुआ
प्रतिवाद - विरोध, खंडन
बंडेर - छाजन के बीचोंबीच लगाया जाने वाला बल्ला जिस पर ठाट का बोझ रहता है
बिसात - बिछाई जाने वाली चीज़
लड़कौंध - छोटी आयु का
साहाय्य - सहायता, मदद, मैत्री
न कूकुर भूँका,
न पहरू जागा - ज़रा सा भी खटका न होना
झक मारना - बेकार बात करना
मुँह लगना - व्यर्थ समय बरबाद करना
खून का घूँट पीकर रह जाना - गुस्से को दबा जाना
सुरखाब का पर लगना - खास बात होना
मुँह में खून लगना - आदत पड़ जाना
खाक छानना - भटकना, खोज करना
पानी-पानी होना - शर्मिंदा होना
छक्के छूटना - घबरा जाना
दिल फड़कना - जोश उत्पन्न करना
नून-मिर्चा लगाना - भड़काना
पी जाना - छिपाना, सहन करना
डेरा डालना - अड्डा जमाना
रुपए में तीन अठन्नी भुनाना - अधिकतम लाभ लेना