Table of Contents

अध्याय 3
सामाजिक संस्थाएँ : निरंतरता एवं परिवर्तन
दूसरे अध्याय मेें भारतीय जनंसख्या की संरचना और गतिशीलता के बारे में पढ़ने के बाद, अब हम सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या, सिर्फ़ अलग-अलग, असंबंधित व्यक्तियों का जमघट नहीं है; परंतु यह विभिन्न प्रकार के अलग-अलग पर आपस में संबंधित वर्गों और समुदायों से बना हुआ एक समाज है। यह समुदाय, सामाजिक संस्थाओं और संबंधों के द्वारा बने हुए हैं और संचालित हैं। इस अध्याय में हम भारतीय समाज की तीन प्रमुख संस्थाओं को विस्तार में पढ़ेंगे, नामतः जाति, जनजाति एवं परिवार।
3.1 जाति एवं जाति व्यवस्था
किसी आम भारतीय नागरिक की तरह आप भी जानते होंगे कि ‘जाति’ एक प्राचीन संस्था है जो कि हज़ारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक हिस्सा है। परंतु इक्कीसवीं सदी में रहने वाले किसी भी भारतवासी की तरह आप यह भी जानते होंगे कि ‘जाति’ केवल हमारे अतीत का नहीं बल्कि हमारे आज का भी एक अभिन्न अंग है। यह दो ‘जातियाँ’, एक जो भारत के अतीत का हिस्सा मानी जाती हैं और दूसरी जो कि भारत के वर्तमान का हिस्सा है, कहाँ तक समान हैं? इस खंड में हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
अतीत में जाति
जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी अनूठी संस्था हैै। हालाँकि विश्व के अन्य भागों में भी समान प्रभाव उत्पन्न करने वाली सामाजिक व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं, परंतु जाति व्यवस्था अपने आप में अपवाद ही है। हालाँकि, यह हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता है पर इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों में भी फैला हुआ है खासकर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में।
माना जाता है कि अंग्रेज़ी के शब्द कास्ट (caste) की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कास्टा (casta) से हुई है। पुर्तगाली कास्टा का अर्थ है विशुद्ध नस्ल। अंग्रेज़ी शब्द कास्ट का अर्थ एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से है जिसे भारतीय भाषाओं में (प्राचीन संस्कृत भाषा से प्रारंभ करते हुए) दो विभिन्न शब्दों-वर्ण और जाति-के अर्थ में उपयोग किया जाता है। वर्ण, जिसका शाब्दिक तात्पर्य है ‘रंग’, समाज के ब्राह्ममण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार श्रेणियों के विभाजन को वर्ण कहा जाता है। हालाँकि इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण भाग शामिल नहीं है जो कि ‘जाति बहिष्कृत’, विदेशियों, दासों, युद्धों मेें पराजित लोगों एवं अन्य लोगों से मिलकर बना है। इन्हें कभी-कभी ‘पंचम’ या पाँचवीं श्रेणी भी कहा जाता है। जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज़ के प्रकार या वंश-किस्म (स्पीशीज) को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अचेतन वस्तुओं से लेकर पेड़-पौधों, जीव-जंतु और मनुष्य भी शामिल होते हैं। भारतीय भाषाओं में जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः जाति संस्था के संदर्भ में ही किया जाता है। हालाँकि यह दिलचस्प है कि भारतीय भाषा बोलने वाले लोग, अंग्रेज़ी शब्द ‘कास्ट’ का प्रयोग भी करनेे लगे हैं।
‘वर्ण’ और ‘जाति’ के आपसी संबंध की सटीक व्याख्या क्या हो? यह प्रश्न विद्वानों के बीच अटकलबाज़ी व बहस का विषय रहा है। सबसे सामान्य व्याख्या यह है कि वर्ण को एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है, वहीं जाति को क्षेत्रीय या स्थानीय उप-वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है जिसमें सैकड़ों या यहाँ तक की हज़ारों जातियों एवं उप-जातियों से बनी अत्यधिक जटिल व्यवस्था शामिल होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ चार वर्णों का वर्गीकरण पूरे भारत में समान है, वहीं जाति अधिक्रम के वर्गीकरण क्षेत्रीय हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं।
इस बात पर भी मतभेद है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सुनिश्चित काल क्या है। सामान्यतः यह माना जाता है कि चार वर्णों का वर्गीकरण लगभग तीन हज़ार साल पुराना है। हालाँकि, विभिन्न समय कालाें में ‘जाति व्यवस्था’ के विभिन्न स्वरूप रहे हैं इसलिए यह मान लेना कि एक समान व्यवस्था तीन हज़ार वर्षों से चली आ रही है अपने आप को भ्रमित करना होगा। अपने प्रारंभिक काल, वैदिक काल, 900-500 ई. पू. के बीच में जाति व्यवस्था वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही थी और इसके केवल चार विभाजन थे। यह विभाजन बहुत विस्तृत या बहुत कठोेर नहीं थे और यह जन्म से निर्धारित नहीं होते थे। इन वर्गों के बीच स्थान परिवर्तन संभव ही नहीं बल्कि सामान्य भी था। अतः उत्तर-वैदिक काल में ही जाति एक कठोर संस्था बनी जिससे हम जाति की प्रसिद्ध परिभाषाओं द्वारा परिचित हैं।
जाति की सबसे सामान्य निर्धारित विशेषताएँ निम्न हैं :
अयन्कली
(1863 - 1914)

अयन्कल्ली का जन्म केरल में हुआ। आप निम्न जातियों एवं दलितों के नेता थे। इनके प्रयासों से, दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाने की आजादी मिली।
1. जाति, जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता-पिता की जाति में ही ‘जन्म लेता’ है। जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होेती। हम अपनी जाति को कभी भी बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते या हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते कि हमें जाति में शामिल होना है या नहीं। हालाँकि, एेसे उदाहरण हैं जहाँ एक व्यक्ति को उसकी जाति से निकाला भी जा सकता है।
2. जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह ‘सजातीय’ होते हैं अर्थात् विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकते हैं।
3. जाति सदस्यता में खाने और खाना बाँटने के बारे में नियम भी शामिल होते हैं। किस प्रकार का खाना खा सकते हैं और किस प्रकार का नहीं, यह निर्धारित है और किसके साथ खाना बाँटकर खाया जा सकता है यह भी निर्धारित होता है।
4. जाति में श्रेणी एवं प्रस्थिति के एक अधिक्रम में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। सैद्धांतिक तौर पर, हर व्यक्ति की एक जाति होती है और हर जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित स्थान होता है। जहाँ अनेक जातियों की अधिक्रमित स्थिति, विशेषकर मध्यक्रम की श्रेणियों में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल सकती है पर अधिक्रम हमेशा पाया जाता है।
5. जातियों में आपसी उप-विभाजन भी होता है अर्थात् जातियों में हमेशा उप-जातियाँ होती हैं और कभी-कभी उप-जातियों में भी उप-उप-जातियाँ होती हैं। इसे खंडात्मक संगठन (segmental organisation) कहते हैं।
6. पारंपरिक तौर पर जातियाँ व्यवसाय से जुड़ी होती थीं। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था, अतः वह व्यवसाय वंशानुगत थे अर्थात् यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। दूसरी ओर, एक विशेष व्यवसाय को किसी जाति सेे जुड़े होने की वजह से उसी जाति के लोग अपना सकते थे, किसी दूसरी जातियों के सदस्य वह काम नहीं कर सकते थे।
यह विशिष्टताएँ निर्धारित नियम हैं जो प्राचीन धर्म-ग्रंथों में पाए जाते हैं। चूँकि यह निर्धारित नियम हमेशा व्यवहार में नहीं थे, हम यह नहीं कह सकते कि यह नियम किस सीमा तक जाति की आनुभविक वास्तविकता अर्थात् उस समय के लोगों के लिए इसका निश्चित अर्थ निर्धारित करते थे। जैसाकि आपके सामने है अधिकांश निर्धारित नियमों में प्रतिबंध शामिल थे। एेतिहासिक सूत्रों से यह भी साफ़ तौर पर साबित होता है कि जाति एक बहुत असमान संस्था थी। जहाँ कुछ जातियों को तो इस व्यवस्था से बहुत लाभ रहा, वहीं अन्य जातियों को इसकी वजह से अधीनता एवं कभी भी न समाप्त होने वाले श्रम का जीवन जीने का दंड भुगतना पड़ा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब जाति जन्म द्वारा कठोरता से निर्धारित हो गई उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए सैद्धांतिक तौर पर कभी भी उसकी जीवन स्थिति बदलना असंभव था। चाहे उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक हों या न हों, उनका स्तर हमेशा उच्च ही रहता था जबकि निम्न जाति के लोगाें का स्तर हमेशा निम्न रहता था।
जोतिराव गोविन्दराव फुले
(1827-1890)

जोतिराव गोविन्दराव फुले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना की और छुआछूत के नियमाें की घोर निंदा की। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जो निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था।
सैद्धांतिक तौर पर, जाति व्यवस्था को सिद्धांतों के दो समुच्चयों के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है, एक भिन्नता और अलगाव पर आधारित है और दूसरा संपूर्णता और अधिक्रम पर। हर जाति से यह अपेक्षित है कि वह दूसरी जाति से भिन्न हों और इसलिए वह प्रत्येक अन्य जाति से कठोरता से पृथक होती है। अतः जाति के अधिकांश धर्मग्रंथसम्मत नियमों की रूपरेखा जातियों को मिश्रित होने से बचाने के अनुसार बनाई गई है। इन नियमों में शादी, खान-पान एवं सामाजिक अंतःक्रिया से लेकर व्यवसाय तक के नियम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर इन विभिन्न एवं पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, वे एक बड़ी संपूर्णता से संबंधित होकर ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। समाज की संपूर्णता में सभी जातियाँ शामिल होती हैं। इससे भी आगे, यह सामाजिक संपूर्णता या व्यवस्था समानतावादी व्यवस्था होने की बजाय अधिक्रमित व्यवस्था है। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ-साथ एक क्रम श्रेणी भी होती है। एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था जो ऊपर से नीचे जाती है, में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है।
धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से जाति की अधिक्रमित व्यवस्था ‘शुद्धता’ (शुचिता) और ‘अशुद्धता’ (अशुचिता) के बीच के अंतर पर आधारित होती है। यह विभाजन जिसे हम पवित्र के करीब मानने में विश्वास रखते हैं (अतः कर्मकांड की शुद्धता के लक्ष्यार्थ), उसके और जिसे हम पवित्र से परे मानते हैैं या उसके विपरीत मानते हैं अतः वह कर्मकांड के लिए प्रदूषित होता है, के बीच हैं। वह जातियाँ जिन्हें कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है उनका स्थान उच्च होता है और जिनको कम शुद्ध या अशुद्ध माना जाता है उन्हें निम्न स्थान दिया जाता है। जैसाकि हर समाज में होता है, सामाजिक स्तर से भौतिक शक्ति (अर्थात्, आर्थिक या सैन्य शक्ति) नज़दीकी से जुड़ी होती है, अतः जिनके पास शक्ति होती है उनकी स्थिति उच्च होती है और जिनके पास शक्ति नहीं होती उनकी स्थिति निम्न होती है। इतिहासकारों का मानना है कि जो लोग युद्धों में पराजित हुए थे उन्हें अक्सर निम्न जाति की स्थिति मिली।
अंत में यह भी कहा जा सकता है कि जातियाँ एक दूसरे से सिर्फ़ कर्मकांड की दृष्टि से ही असमान नहीं हैं; उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे एक-दूसरे की सहयोगी होंगी एवं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक जाति का व्यवस्था में अपना स्थान तय है और वो स्थान किसी भी अन्य जाति को नहीं दिया जा सकता। चूँकि, जाति व्यवसाय से भी जुड़ी हुई है, अतः व्यवस्था श्रम के सामाजिक विभाजन के अनुरूप कार्य करती है, परंतु सैद्धांतिक तौर पर यह किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता की अनुमति नहीं देती है।
यह अचंभे की बात नहीं है कि अतीत के बारे में हमारे ज्ञान के स्रोत, मुख्यतः प्राचीन काल के बारे में, अपर्याप्त हैं। यह तय कर पाना मुश्किल है कि उस समय परिदृश्य कैसा था या किन कारणों से कुछ संस्थाओं या व्यवहारों की स्थापना हुई थी। परंतु, अगर हमें इस बारे में पूरी जानकारी होती तोे भी उससे हमें यह नहीं पता चल सकता कि आज हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ़ इसलिए कि अतीत में कुछ हुआ था वह हमारी परंपरा का हिस्सा है; यह आवश्यक नहीं कि वह हमेशा के लिए सही या गलत है। प्रत्येक काल में इन प्रश्नों के बारे में नए सिरे से सोचना होगा और अपनी सामाजिक संस्थाओं के बारे में स्वयं के सामूहिक निर्णय को बनाना होगा।
सावित्री बाई फुले
(1831-1897)

सावित्री बाई फुले देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थीं जो पुणे में स्थापित किया गया था। इन्होंने अपना पूरा जीवन शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा अर्पण करने में लगा दिया। इन्होंने किसानों और मज़दूरों के लिए रात्रि विद्यालयों की शुरुआत की। इनकी मृत्यु प्लेग से पीड़ित मरीज़ों की देखभाल के दौरान हुई।
उपनिवेशवाद और जाति
प्राचीन काल की तुलना में, हम अपने हाल के इतिहास में जाति के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। यदि यह माना जाए कि आधुनिक इतिहास 19वीं शताब्दी के साथ प्रारंभ हुआ तो 1947 में प्राप्त भारतीय स्वतंत्रता को औपनिवेशिक काल (मोटे तौर पर 1800 से 1947 तक के लगभग 150 वर्ष) और स्वातंत्र्योत्तर अथवा औपनिवेशिक शासन के बाद के काल (1947 से आज तक के छह दशक) के बीच स्वाभाविक विभाजक रेखा मान सकते हैं। एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और साथ ही स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से हुए परिवर्तनों द्वारा मज़बूती से आकार प्रदान किया गया।
विद्वज्जन इस बात पर सहमत हैं कि औपनिवेशिक काल के दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन आए। वस्तुतः कुछ विद्वान तो कहते हैं कि आज जिसे हम जाति के रूप में जानते हैं वह प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की ही अधिक देन है। यह सभी परिवर्तन जान-बूझकर या सोच-समझकर नहीं लाए गए। प्रारंभ में, ब्रिटिश प्रशासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करना सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्थाओं की जटिलताओं को समझने के प्रयत्न शुरू किए। इन प्रयत्नों के अंतर्गत देश भर में विभिन्न जनजातियों तथा जातियों की ‘प्रथाओं और तौर-तरीकों’ के बारे में अत्यंत सुव्यवस्थित रीति से गहन सर्वेक्षण किए गए और उनके विषय में रिपोर्टें तैयार की गईं। अनेक ब्रिटिश प्रशासक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ-साथ शौकिया तौर पर नृजातिविज्ञानी भी थे और उन्होंने सर्वेक्षण तथा अध्ययन कार्यों में बहुत रुचि ली।
लेकिन जाति के विषय में सूचना एकत्र करने का अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रयत्न जनगणना के माध्यम से किया गया। जनगणना के कार्य को सर्वप्रथम 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद 1881 से तो जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियमित रूप से हर दस वर्ष बाद कराई जाने लगी। 1901 में हरबर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया गया अर्थात् किस क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊँचा या नीचा स्थान प्राप्त है और तदनुसार श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई। जाति के सामाजिक बोध पर इस प्रयास का गहरा प्रभाव पड़ा और विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा जनगणना आयुक्त के पास सैकड़ों याचिकाएँ भेजी गईं जिनमें उन्होंने सामाजिक क्रम में अपनी जाति को अधिक ऊँचा स्थान देने की माँग की थी और अपने दावों के समर्थन में अनेक एेतिहासिक तथा धर्मशास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए थे। कुल मिलाकर, विद्वान यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार की जातीय गणना और आधिकारिक रूप से जातियों की प्रस्थिति का अभिलेख करने के प्रत्यक्ष प्रयास ने जाति संस्था के स्वरूप को ही बदल डाला। इस प्रकार के हस्तक्षेप से पहले जातियों की पहचान अपेक्षाकृत बहुत अधिक अस्थिर तथा कम कठोर थी। जब एक बार उनकी गणना प्रारंभ हो गई और उसे अभिलिखित किया जाने लगा तो फिर जाति का एक नया जीवन प्रारंभ हो गया।
पेरियार (ई.वी. रामास्वामी नायकर)
(1879-1973)
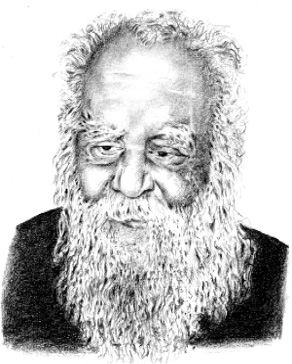
पेरियार (ई. वी. रामास्वामी नायकर) एक बुद्धिवादी और दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लोगों को यह महसूस करने के लिए उद्बोधित किया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले।
औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए अन्य हस्तक्षेपों ने भी इस संस्था पर अपना प्रभाव डाला। भूराजस्व व्यवस्थाओं और तत्संबंधी प्रबंधों तथा कानूनों ने उच्च जातियों के रूढ़िगत (जाति आधारित) अधिकारों को वैध मान्यता देने का कार्य किया। अब ये जातियाँ, सामंती वर्गों की बजाय, आधुुनिक अथोेρं में भू-स्वामी यानी ज़मीन की मालिक बन गईं और ज़मीन की उपज पर अथवा राजस्व या अन्य कई प्रकार के नज़रानों पर उनका दावा स्थापित हो गया। पंजाब की तरह अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाएँ प्रारंभ की गईं और उनके साथ-साथ लोगों को वहाँ बसाने के प्रयत्न किए गए और इन सभी प्रयत्नों का भी अपना एक जातीय आयाम था। इस क्रम के दूसरे सिरे पर औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में, प्रशासन ने पददलित जातियों, जिन्हें उन दिनों ‘दलित वर्ग’ कहा जाता था, के कल्याण में भी रुचि ली। इन प्रयत्नों के अंतर्गत ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूचियों या ‘अनुसूचियों’ को वैध मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार, ‘अनुसूचित जनजातियाँ’ और ‘अनुसूचित जातियाँ’ शब्द अस्तित्व में आए। जातीय अधिक्रम में जो जातियाँ सबसे नीचे थीं जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाव बरता जाता था और जिनमें सभी तथाकथित ‘अस्पृश्य’ यानी अछूत जातियाँ शामिल थीं, उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। (आप आगे सामाजिक अपवर्जन विषयक पाँचवेें अध्याय में अस्पृश्यता और उसके विरुद्ध संघर्ष के बारेे में और अधिक पढ़ेंगे)।
इस प्रकार, उपनिवेशवाद ने जाति संस्था में अनेक प्रमुख परिवर्तन किए। शायद यह कहना अधिक समीचीन होगा कि औपनिवेशिक काल में जाति संस्था में अनेक आधारभूत परिवर्तन आए। उस काल में, पूँजीवाद और आधुनिकता के प्रसार के कारण, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में तेज़ी से बदलाव आ रहा था।
जाति का समकालीन रूप
1947 में भारत को प्राप्त स्वतंत्रता वैसे तो एक बहुत बड़ी घटना थी पर उसके बाद भी भारत को अपने औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला। राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए व्यापक पैमाने पर जनमत जुटाने में भी जातीय भावनाओं एवं आधारों ने अनिवार्य रूप से अपनी भूमिका अदा की थी। ‘दलित वर्गों’ और विशेष रूप से अस्पृश्य (अछूत) समझी जाने वाली जातियों को संगठित करने के प्रयत्न राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रारंभ हो चुके थे। जातीय अधिक्रम के दोनों सिरों से उच्च कही जाने वाली जातियों के प्रगतिशील सुधारकों और नीची समझी जाने वाली जातियों के सदस्यों जैसे, पश्चिमी भारत में महात्मा जोतिबा फुले और बाबा साहेब अंबेडकर और दक्षिण भारत में अय्यनकालि, श्री नारायण गुरू, इयोतीदास और पेरियार (ई. वी. रामास्वामी नायकर) दोनों ने ही इस दिशा में पहल की। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर दोनों ने ही 1920 के दशक से अस्पृश्यता (छुआछूत) के विरुद्ध अपने विरोधांदोलन शुरू कर दिए थे। अस्पृश्यता-विरोधी कार्यक्रमों को कांग्रेस की कार्यसूची में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया और जब स्वतंत्रता क्षितिज पर दृष्टिगोचर होने लगी तब तक राष्ट्रवादी आंदोलन के संपूर्ण परिदृश्य में, मोटे तौर पर यह सहमति हो गई कि जातीय विभिन्नताओं का उन्मूलन कर दिया जाए। राष्ट्रवादी आंदोलन में मुखरित यह प्रबल दृष्टिकोण जाति को एक सामाजिक कुरीति और भारतीयों के बीच फूट डालने की एक औपनिवेशिक युक्ति मानता था। लेकिन राष्ट्रवादी नेतागण, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे, सबसे नीची समझी जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए अस्पृश्यता तथा अन्य जातीय प्रतिबंधों के उन्मूलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहे और साथ ही, भू-स्वामी उच्च जातियों को यह आश्वासन देने में भी सफल रहे कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।
श्री नारायण गुरू
(1856-1928)
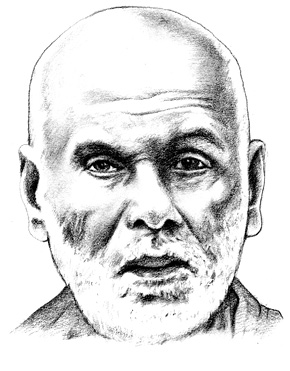
केरल में जन्मे श्री नारायण गुरू ने सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया और जाति व्यवस्था के कुप्रभावों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन सार्थक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया और ‘सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर’ का नारा दिया।
स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्य को ये अंतर्विरोध विरासत में मिले जो बाद में प्रतिबिंबित होते रहे। एक ओर तो राज्य जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था और भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया। दूसरी ओर, राज्य उन आमूलचूल सुधारों को लाने में असमर्थ एवं अनिच्छुक था जो जातीय असमानता के लिए आर्थिक आधार को दुर्बल बना देते। एक अन्य स्तर पर भी, राज्य ने यह माना कि यदि वह जाति प्रथा की ओर आँखें बंद करके काम करेगा तो उससे स्वतः ही जाति आधारित विशेषाधिकार कमज़ोर पड़ जाएँगे और अंततोगत्वा इस संस्था का उन्मूलन हो जाएगा। उदाहरण के लिए, सरकारी पदों पर नियुक्तियों के मामले में जाति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और इस प्रकार अच्छी तरह से शिक्षित उच्च जातियों और अल्प-शिक्षित अथवा अक्सर निरक्षर निम्न जातियों को ‘समान’ आधार पर प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। इसका एकमात्र अपवाद यही था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पद आरक्षित होते थे। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता-प्राप्ति के ठीक बाद के कुछ दशकों तक राज्य ने इस तथ्य पर समुचित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए कि उच्च जातियाँ तथा निम्न समझी जाने वाली जातियाँ आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से कतई समान नहीं हैं।
राज्य के विकास संबंधी कार्यकलाप और निजी उद्योग की संवृद्धि ने भी आर्थिक परिवर्तन में तीव्रता और गहनता लाकर अप्रत्यक्ष रूप से जाति संस्था को प्रभावित किया। आधुनिक उद्योग ने सभी प्रकार के नए-नए रोज़गार के अवसर तैयार किए जिनके लिए कोई जातीय नियम नहीं थे। नगरीकरण और शहरों में सामूहिक रहन-सहन की परिस्थितियों ने सामाजिक अंतःक्रिया के जाति-पृथक्कृत स्वरूपों का अधिक समय तक चलना मुश्किल कर दिया। एक अन्य स्तर पर, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय व्यक्तिवाद और योग्यतातंत्र अर्थात् योग्यता को महत्व देने के उदार विचारों से आकर्षित हुए और उन्होंने अधिक अतिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर, यह भी उल्लेखनीय था कि जाति व्यवस्था कितनी लचीली साबित हुई। औद्योगिक नौकरियों में भर्ती, चाहें वह भर्ती मुंबई की कपड़ा मिलों में हो या कोलकाता की जूट मिलों में अथवा कहीं अन्यत्र हो, जाति और नातेदारी के आधार पर होती रही। बिचौलिया जो कारखानों या मिलों के लिए मज़दूर भर्ती करता था, अपनी जाति या क्षेत्र के उम्मीदवारों में से मज़दूर चुनता था जिससे उन विभागों या कारखानों में अक्सर एक खास जाति के मज़दूरों का ही बोलबाला रहता था। अछूतों के प्रति खूब भेदभाव बरता जाता था और शहरों में भी इस तरह के पूर्वाग्रह का अभाव नहीं था हालाँकि, यह गाँवों की तुलना में कम था।
यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जाति सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में ही सबसे सुदृढ़ सिद्ध हुई। अंतर्विवाह यानी अपनी जाति के भीतर विवाह करने की परिपाटी, आधुनिकीकरण और परिवर्तन से बड़े तौर पर अप्रभावित रही। आज भी अधिकांश विवाह जाति की परिसीमाओं के भीतर ही होते हैं हालाँकि, अंतर्जातीय विवाह अब पहले की तुलना में अधिक हो रहे हैं। किंतु कुछ परिसीमाएँ अधिक लचीली हो गई हैं अथवा उनमें कुछ दरारें पड़ गई हैं, परंतु समान सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति के जाति के समूहों के बीच के विभाजन को बनाए रखने की अब भी बराबर कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, उच्च जातियों (जैसे, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत) के भीतर अंतर्जातीय विवाह संभवतः पहले से कहीं अधिक हो रहे हैं पर उच्च जाति और पिछड़ी या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच विवाह आज भी न के बराबर ही हो रहे हैं। भोजन को मिल-बाँटकर खाने के नियमों के मामले में भी स्थिति लगभग एेसी ही है।
संभवतः परिवर्तन का सबसे घटनापूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र रहा है। स्वतंत्र भारत में अपने प्रारंभ से ही, लोकतांत्रिक राजनीति गहनता से जाति आधारित रही है। हालाँकि इसके आधार पर कार्य करना जटिल से जटिलतर होता गया है और उसके भविष्य के बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जाति चुनावी राजनीति का केेंद्र-बिंदु बनी हुई है। 1980 के दशक से तो हमने स्पष्ट रूप से जाति आधारित राजनीतिक दलों को भी उभरते देखा है। प्रारंभिक सामान्य चुनावों में एेसा प्रतीत हुआ कि जातीय भाईचारे की भूमिका चुनाव जीतने में निर्णायक रही थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही स्थिति अत्यंत जटिल हो गई क्योंकि भिन्न-भिन्न दलों ने जातीय आधार पर मत प्राप्त करने की संभावना का हिसाब लगाने में एक-दूसरे से होड़ शुरू कर दी।
परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं को आजमाने और समझने के लिए समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानवविज्ञानियों ने कई नई-नई संकल्पनाएँ गढ़ीं। शायद उन संकल्पनाओं में सबसे अधिक प्रचलित संकल्पनाएँ ‘संस्कृतिकरण’ और ‘प्रबल-जाति’ की हैं, ये दोनों संकल्पनाएँ एम. एन. श्रीनिवास की देन हैं लेकिन इन पर अन्य विद्वानों द्वारा गहनता से चर्चा और आलोचना की गई है।
‘संस्कृतिकरण’ एक एेसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा (आमतौर पर मध्य या निम्न) जाति के सदस्य किसी उच्च जाति (या जातियों) की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक प्रस्थिति को ऊँचा करने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि यह प्रघटना काफ़ी पुरानी है और स्वतंत्रता-प्राप्ति, यहाँ तक कि औपनिवेशिक काल के भी पहले से अपनाई जाती रही है, लेकिन हाल के समय में इसका बहुत अधिक प्रचार हो गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समानुकरण के लिए अक्सर ब्राह्मण या क्षत्रिय जातियों के रीति-रिवाजों या परिपाटियों को अपनाया जाता था जैसे, शाकाहारी बन जाना, यज्ञोपवीत धारण करना, कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रार्थनाएँ करना और धार्मिक उत्सव मनाना आदि-आदि। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आमतौर पर संबंधित जाति के आर्थिक स्तर में उन्नति होने के बाद या उसके साथ-साथ अपनाई जाती है, यद्यपि यह स्वतंत्र रूप से भी अपनाई जा सकती है। बाद में हुए शोध के फलस्वरूप इस संकल्पना में अनेक संशोधन हो चुके हैं एवं इस संकल्पना के संशोधित संस्करण के लिए सुझाव दिए जा चुके हैं। इनमें यह तर्क भी शामिल है कि संस्कृतिकरण पहले से निषिद्ध किसी अनुष्ठान (कर्मकांड)/सामाजिक विशेषाधिकारों (जैसे, निम्न जाति के लोगों द्वारा यज्ञोपवीत धारण करना, जिसके लिए पहले कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था थी) का अवज्ञापूर्ण दावा हो सकता है न कि ‘निम्न’ जातियों द्वारा ‘उच्च’ जातियों का चाटुकारीपूर्ण अनुकरण।
‘प्रबल जाति’ शब्द का प्रयोग एेसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती थी और जिन्हें स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार प्रदान किए गए थे। इन भूमि-सुधारों ने पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिए थे। ये दावेदार ऊँची जातियों के एेसे सदस्य होते थे जो इस अर्थ में ‘अनुपस्थित यानी दूरवासी ज़मींदार’ थे कि वे अपना लगान वसूल करने के अलावा खेतिहर अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका अदा नहीं करते थे। वे अक्सर उस गाँव में भी नहीं रहते थे बल्कि उनका आवास कस्बों या शहरों में होता था। अब ये भूमि-अधिकार उस अगले स्तर के दावेदारों को प्राप्त हो गए हैं जो कृषि के प्रबंध में तो शामिल थे पर स्वयं भूमि नहीं जोतते थे। ये मध्यवर्ती जातियाँ भी स्वयं परिश्रम नहीं करती थीं, बल्कि भूमि की जुताई, देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मज़दूरों पर आश्रित थीं, जिनमें विशेष रूप से ‘अछूत’ जातियों के मज़दूर शामिल थे। किंतु एक बार जब उन्हें भूमि-अधिकार मिल गए तो फिर उन्होंने पर्याप्त आर्थिक शक्ति प्राप्त कर ली। उनकी बड़ी संख्या ने भी सर्वजनीन वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र के इस युग में उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान की। इस प्रकार, यह मध्यवर्ती जातियाँ देहाती इलाकों में प्रबल जातियाँ बन गईं और क्षेत्रीय राजनीति तथा खेतिहर अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका अदा करने लगीं। इन प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण हैंः बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के वोक्कलिंग, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्मा लोग, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पाटीदार।
मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास
(1916-1999)

मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास, भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री और सामाजिक मानवविज्ञानी हैं। वे जाति व्यवस्था पर किए गए कार्य तथा ‘संस्कृतिकरण’ एवं ‘प्रबल जाति’ जैसे शब्दों के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताब द रिमेम्बरड विलेज सामाजिक मानवविज्ञान में गाँवों में किए गए सबसे अच्छे अध्ययनों में से एक है।
समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में हुए अत्यंत महत्त्वपूर्ण फिर भी विरोधाभासी परिवर्तनों में से एक परिवर्तन यह है कि अब जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय मध्यम और उच्च वर्गों के लिए ‘अदृश्य’ होती जा रही है। इन समूहों के लिए, जो स्वातंत्र्योत्तर काल की विकासात्मक नीतियों से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, जातीयता का महत्त्व सचमुच कम हो गया प्रतीत होता है क्योंकि अब इसका कार्य भलीभाँति संपन्न हो चुका है। इन समूहों की जातीय प्रस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रही है कि इन समूहों को तीव्र विकास द्वारा प्रदत्त अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक आर्थिक तथा शैक्षिक संसाधन उपलब्ध हों। खासतौर पर, ऊँची जातियों के संभ्रांत लोग आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान तथा प्रबंधन में व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित होने में सफल हुए। इसके साथ-साथ, वे स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में राजकीय क्षेत्र की नौकरियों में हुए विस्तार का भी लाभ उठा सकें। इस प्रारंभिक अवधि में, शेष समाज की तुलना में उनकी अग्रणी स्थिति (शिक्षा की दृष्टि से) ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें किसी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी दूसरी तथा तीसरी पीढ़ियों में जब उनकी विशेषाधिकार प्राप्त प्रस्थिति और सुदृढ़ हो गई तब इन समूहों को यह विश्वास होने लगा कि उनकी प्रगति का जाति से कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं था। निश्चित रूप से, इन समूहों की तीसरी पीढ़ियों के लिए उनकी आर्थिक तथा शैक्षिक पूँजी अकेले ही यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है कि उन्हें जीवन में सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होते रहेंगे। इस समूह के लिए, सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई भूमिका नहीं रही है, वह धार्मिक रीति-रिवाज, विवाह अथवा नातेेदारी के व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित है। किंतु, यह एक विशेषीकृत या विभेदित समूह है और इस तथ्य ने आगे एक और जटिलता उत्पन्न कर दी है। यद्यपि विशेषाधिकार या सुविधा प्राप्त इस समूह में ऊँची जाति के लोगों का ही बाहुल्य है, लेकिन ऊँची जातियों के सभी लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है, उनमें से कुछ लोग गरीब भी हैं।
जहाँ तक तथाकथित अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का संबंध है, उनके लिए तो उपर्युक्त से विपरीत स्थिति ही घटित हुई है। उनके लिए, जाति और अधिक दिखने वाली हो गई, निस्संदेह उनकी जाति ने उनकी पहचान के अन्य सभी आयामों को ग्रस लिया है। क्योंकि उन्हें विरासत में कोई शैक्षिक और सामाजिक पूँजी नहीं मिली है और उन्हें पहले से संस्थापित उच्च जाति समूह के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ रहा है। इसलिए वे अपनी जातीय पहचान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनकी बहुत थोड़ी सी सामूहिक परिसंपत्तियों में से एक है। इसके आगे, वे अभी भी विभिन्न प्रकार के भेदभाव के शिकार हैं। आरक्षण की नीतियाँ और राजनीतिक दबाव में आकर राज्य द्वारा उन्हें दिए गए अन्य संरक्षण ही उनके जीवन को बचाने वाले उपाय हैं। परंतु इन जीवन रक्षक साधनों का उपयोग करना ही उनकी जाति को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बना देता है और अक्सर यही उनकी पहचान का वह पक्ष होता है जिसे दुनिया मान्यता देती है।
इस प्रकार जाति रहित प्रतीत होने वाला उच्च जातीय समूह और प्रत्यक्ष रूप से जाति परिभाषित निम्न जातीय समूह इन दोनों समूहों का सन्निकट होना (पास-पास होना) ही आज की जाति संस्था का एक केंद्रीय पक्ष है।
3.2 जनजातीय समुदाय
जनजाति एक आधुनिक शब्द है जो एेसे समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं और उप-महाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं। भारत में जनजातियों की परिभाषा नकारात्मक शब्दों में अर्थात् वे क्या नहीं हैं यह बताकर की जाती है। जनजातियाँ एेसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्मग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे; उनका कोई सामान्य प्रकार का राज्य या राजनीतिक संगठन नहीं था; उनके समुदाय कठोर रूप में वर्गों में नहीं बँटे हुए थे; और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी; न वे हिंदू थे और न ही किसान। ‘जनजाति’ शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक युग में प्रारंभ किया गया था। समुदायाें के एक अत्यंत विषम समुच्चय के लिए एक अकेले शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही किया गया था।
जनजातीय समाजों का वर्गीकरण
जहाँ तक सकारात्मक विशिष्टताओं का संबंध है, जनजातियों को उनके ‘स्थायी’ तथा ‘अर्जित’ विशेषकों के अनुसार विभाजित किया गया है। स्थायी विशेषकों या लक्षणों में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टताएँ और पारिस्थितिक आवास शामिल हैं।
स्थायी विशेषक
भारत की जनजातीय जनसंख्या व्यापक रूप से बिखरी हुई है लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनकी आबादी काफी घनी है। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85% भाग ‘मध्य भारत’ में रहता है जो पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है और जिसके हृदय-स्थल (मध्य भाग) में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भाग स्थित हैं। जनजातीय जनसंख्या के शेष 15% में से 11% से अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में और बाकी के 3% से थोड़े-से अधिक शेष भारत में रहते हैं। यदि हम राज्य की जनसंख्या में जनजातियों के हिस्से पर दृष्टिपात करें तो पाएँगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी आबादी सबसे घनी है; वहाँ असम को छोड़कर सभी राज्यों में उनका घनत्व 30% से अधिक है और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में तो जनजातीय आबादी 60% से अधिक और 95% तक है। किंतु, देश के शेष भागों में जनजातीय जनसंख्या बहुत छोटी है यानी उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 12% से कम है। इनके पारिस्थितिक आवासों में पहाड़ियाँ, वन, ग्रामीण मैदान और नगरीय औद्योगिक इलाके शामिल हैं।
भाषा की दृष्टि से, जनजातियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से दो श्रेणियों अर्थात् भारतीय-आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएँ शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा भी बोली जाती हैं और जनजातियों में से लगभग 1% लोग ही भारतीय आर्य परिवार की भाषाएँ और लगभग 3% लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएँ बोलते हैं। दो अन्य भाषा समूह, आस्ट्रिक और तिब्बती-बर्मी, प्राथमिक रूप से जनजातीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं, जिनमें से आस्ट्रिक परिवार की भाषाएँ पूर्ण रूप से जनजातीय लोगों द्वारा और तिब्बती-बर्मी परिवार की भाषाएँ 80% से अधिक जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। शारीरिक-प्रजातीय दृष्टि से, जनजातियों का नीग्रिटो, आस्ट्रैलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। भारत की जनसंख्या का शेष भाग भी द्रविड़ और आर्य श्रेणियों के अंतर्गत आता है।
जनसंख्या के आकार की दृष्टि से, जनजातियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या लगभग 70 लाख है जबकि सबसे छोटी जनजाति यानी अंडमान द्वीपवासियों की जनसंख्या शायद 100 व्यक्तियों से भी कम है। सबसे बड़ी जनजातियाँ गाेंड, भील, संथाल, ओराँव, मीना, बोडो और मुंडा हैं, इनमें से सभी की जनसंख्या कम-से-कम दस लाख है। जनजातियों की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की समस्त जनसंख्या का लगभग 8.2% या लगभग 8.4 करोड़ व्यक्ति हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियाँ भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है अथवा लगभग 104 मिलियन जनजातीय लोग इस देश में निवास करते हैं।
अर्जित विशेषक
अर्जित विशेषकों पर आधारित वर्गीकरण दो मुख्य कसौटियों आजीविका के साधन और हिंदू समाज में उनके समावेश की सीमा अथवा दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है।
आजीविका के आधार पर, जनजातियों को मछुआ, खाद्य संग्राहक और आखेटक (शिकारी), झूम खेती करने वाले, कृषक और बागान तथा औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। लेकिन अकादमिक समाजशास्त्र और राजनीति तथा सार्वजनिक मामलों में अपनाए जाने वाले सबसे प्रभावी वर्गीकरण इस बात पर आधारित हैं कि हिंदू समाज में अमुक जनजाति को कहाँ तक आत्मसात् किया गया है। इस आत्मसात्करण को जनजातियों के दृष्टिकोण से अथवा (जैसाकि अक्सर होता है) प्रबल हिंदू मुख्यधारा के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जनजातियों के दृष्टिकोण से, आत्मसात्करण की सीमा के अलावा, हिंदू समाज के प्रति अभिवृत्ति (रुख) भी एक बड़ी कसौटी है क्योंकि जनजातियों की अभिवृत्तियों के बीच काफ़ी अंतर होता है–कुछ जनजातियों का हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव होता है जबकि कुछ जनजातियाँ उसका प्रतिरोध या विरोध करती हैं। मुख्यधारा के दृष्टिकोण से, जनजातियों को हिंदू समाज में मिली प्रस्थिति की दृष्टि से भी देखा जा सकता है जिसमें कुछ को तो ऊँचा स्थान दिया जाता है पर अधिकांश को आमतौर पर नीचा स्थान ही मिलता है।
जनजाति : एक संकल्पना की जीवनी
1960 के दशक में विद्वानों के बीच इस प्रश्न को लेकर वाद-विवाद होता रहा कि क्या जनजातियों को जाति आधारित (हिंदू) कृषक समाज के एक सिरे का विस्तार माना जाए अथवा वे पूर्ण रूप से एक भिन्न प्रकार का समुदाय है। जो विद्वान विस्तार के पक्ष में थे उनका कहना था कि जनजातियाँ जाति आधारित कृषक समाज से मौलिक रूप से भिन्न नहीं हैं, लेकिन उनमें स्तरीकरण बहुत कम हुआ है (अधिक्रम के स्तर कम हैं) और संसाधनों के स्वामित्व के मामले में वे समुदाय आधारित अधिक और व्यक्ति आधारित कम हैं। किंतु, उनके विरोधी पक्ष का कहना था कि जनजातियाँ जातियों से पूरी तरह भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता का भाव नहीं होता जो कि जाति व्यवस्था का केंद्र-बिंदु है।

संक्षेप में, जनजाति और जाति के बीच के अंतर को दर्शाने वाला तर्क पवित्रता और अपवित्रता और अधिक्रमिक एकीकरण में विश्वास रखने वाली हिंदू जातियों और अपेक्षाकृत अधिक समतावादी और नातेदारी आधारित सामाजिक संगठन की रीतियों वाली जीववादी (animist) जनजातियों के बीच माने गए सांस्कृतिक अंतर पर आधारित था।
1970 के दशक तक आते-आते, जनजाति की सभी प्रमुख परिभाषाएँ दोषपूर्ण दिखाई देने लगीं। यह दर्शाया गया कि जनजाति और कृषक समुदाय के बीच किया गया अंतर सामान्य रूप से अपनाई गई कसौटियों–आकार, पृथक्करण, धर्म और आजीविका के साधनों में से किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। संथाल, गोंड और भील जैसी कुछ भारतीय ‘जनजातियाँ’ बहुत बड़ी हैं और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं। मुंडा, हो जैसी कुछ अन्य जनजातियाँ काफ़ी समय से एक स्थान पर बसकर खेती करने लगीं हैं और यहाँ तक कि बिहार की बिरहोर जैसी शिकारी-संग्राहक जनजातियों ने भी विशेष प्रकार के घर बसा लिए हैं जहाँ रहकर वे टोकरियाँ बुनती हैं और तेल निकालने जैसे अन्य कार्य करती हैं। कुछ अनेक मामलों में यह भी इंगित किया गया है कि अन्य विकल्पों के अभाव में, ‘जातियों’ (या गैर जनजातीय लोगों) ने शिकार और संग्रहण का पेशा अपना लिया है।
जाति और जनजाति के बीच के अंतरों पर जो चर्चा हुई उसके साथ ही उन प्रक्रियाओं तथा उपायों के विषय में काफ़ी बड़ा साहित्य तैयार किया गया जिनके माध्यम से भिन्न-भिन्न युगों में जनजातियों को हिंदू समाज में आत्मसात् किया गया। ये प्रक्रियाएँ थींः संस्कृतिकरण, सवर्ण हिंदुओं द्वारा विजय के बाद विजितों को शूद्रवर्णों के अंतर्गत शामिल करना, परसंस्कृतिग्रहण (acculturation) और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा। भारतीय इतिहास के संपूर्ण विस्तार में यह अक्सर देखने को मिलता है कि विभिन्न जनजातीय समूहों को हिंदू समाज के जातीय अधिक्रम में विभिन्न स्तरों पर आत्मसात् कर लिया गया, क्योंकि ज़मीनों पर बस्तियाँ बसा दी गईं और जंगलों का सफाया कर दिया गया। इसे या तो स्वाभाविक तथा समानांतर प्रक्रिया के रूप में देखा गया जिसके द्वारा सभी समूहों का पंथों के रूप में हिंदुत्व में आत्मसात्मीकरण कर लिया गया या इसे शोषणात्मक प्रक्रिया माना गया। मानवविज्ञानियों की प्रारंभिक शाखा के लेखकों ने मुख्यधारा में जनजातियों के समावेश के सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक बल दिया जबकि परवर्ती लेखकों ने सम्मिलित करने के शोषणात्मक तथा राजनीतिक स्वरूप पर अपना लेखन केंद्रित किया है।
कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जनजातियों को एेसे ‘आदिम’ (prestine) अर्थात् मौलिक अथवा विशुद्ध-समाज, जो सभ्यता से अछूते रहेे हों, मानने का कोई सुसंगत आधार नहीं है। इसके स्थान पर उनका यह प्रस्ताव है कि जनजातियों को वास्तव में एेसी ‘द्वितीयक’ प्रघटना माना जाए जो पहले से विद्यमान राज्यों और जनजातियों जैसे राज्येतर समूहों के बीच शोषणात्मक और उपनिवेशवादी संपर्क के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। एेसा संपर्क स्वयं ही एक ‘जनजातिवादी’ विचारधारा को जन्म देता है–जनजातीय समूह नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने-आपको अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं।
फिर भी यह आम धारणा कि जनजातीय समुदाय उन प्रस्तर युगीन आखेटक और संग्राहक समाजों के समान हैं जो सामयिक परिवर्तनों से अछूते रहे हैं अभी भी सामान्य तौर पर विद्यमान है हालाँकि, काफ़ी लंबे समय से यह सच नहीं रहा है। आइए, सर्वप्रथम आदिवासियों पर ही विचार करें, आदिवासी लोग सदा इतने पीड़ित समूह नहीं थे जितने वे आज हैं। मध्य भारत में अनेक गाेंड राज्य रहे हैं जैसे, गढ़ मांडला या चाँदा। मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भारत के तथाकथित राजपूत राज्यों में से अनेक रजवाड़े वास्तव में स्वयं आदिवासी समुदायों में स्तरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही उत्पन्न हुए। आदिवासी लोग अक्सर अपनी आक्रामक क्षमता और स्थानीय सैन्य दलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से मैदानी इलाकों के लोगों पर अपने प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा, वे कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का व्यापार भी करते थे जिसके अंतर्गत वे वन्य उत्पाद, नमक और हाथी बेचा करते थे। इसके अतिरिक्त, जब वन्य संसाधनों और खनिजों का दोहन करने और सस्ते श्रमिकों की भर्ती करने के लिए पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अभियान चला तो उसने काफ़ी समय पहले जनजातीय समाजों को मुख्यधारा वाले समाज के संपर्क में ला दिया।
मुख्यधारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति रवैया
हालाँकि, औपनिवेशिक युग की प्रारंभिक मानववैज्ञानिक कृतियों में जनजातियों को एकाकी असंपृक्त समुदायों के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन उपनिवेशवाद उनकी दुनिया में पहले ही अटल परिवर्तन ला चुका था। राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर, जनजातीय समाजों को पैसा उधार देने वाले तथाकथित साहूकारों की घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही, वे गैर-जनजातीय अप्रवासी, एक जगह पर बस जाने वाले लोगों के हाथों अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे और वनों के आरक्षण की सरकारी नीति और खनन कार्यों का प्रारंभ हो जाने से वनों तक उनकी पहुँच भी खत्म होती जा रही थी। अन्य इलाकों के विपरीत, जहाँ भूमि का लगान ही अतिरिक्त आय का प्राथमिक स्रोत था, इन पहाड़ी और जंगली इलाकों में, वनों और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विनियोजन ही अधिकतर औपनिवेशिक सरकार के लिए आय का प्रमुख स्रोत था। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में जनजातीय इलाकों में अनेक विद्रोह हो जाने के बाद, औपनिवेशिक सरकार ने ‘अपवर्जित’ (excluded) और ‘आंशिक अपवर्जित’ (partially exluded) इलाके निर्धारित घोषित कर दिए जहाँ गैर-जनजातीय लोगों का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध या विनियमित था। ब्रिटिश सरकार इन इलाकों में स्थानीय राजाओं या मुखियाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाने के पक्ष में थी।
1940 के दशक में पृथक्करण (isolation) बनाम एकीकरण (integration) विषय पर जो प्रसिद्ध वाद-विवाद चला वह जनजातीय समाजों की पृथक हुई संपूर्ण अस्तित्व की मानक तस्वीर पर ही आधारित था। पृथकतावादी पक्ष का कहना था कि जनजातीय लोगों को व्यापारियों, साहूकारों और हिंदू तथा ईसाई धर्मप्रचारकों से बचाए रखने की आवश्यकता है क्यों ये सभी लोग जनजातियों का अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर, एकीकरणवादी पक्ष का कहना था कि जनजातीय लोग पिछड़े हुए हिंदू ही हैं और उनकी समस्याओं का समाधान उसी परिधि के भीतर खोजा जाए जो अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में निर्धारित की गई है। इस विरोधी पक्ष का संविधान सभा के वाद-विवादों में बोलबाला रहा और अंततः समझौते के तौर पर यह तय किया गया कि जनजातियों के कल्याण के लिए एेसी योजनाएँ बनाई जाएँ जिनके माध्यम से उनका नियंत्रित एकीकरण संभव हो जाए। इसलिए बाद में जनजातीय विकास की जो भी योजनाएँ बनाई गईं जैसे, पंचवर्षीय योजनाएँ, जनजातीय उप-योजनाएँ, जनजातीय कल्याण खंड, विशेष बहुप्रयोजनी क्षेत्र योजनाएँ, वे सभी इसी सोच पर आधारित रही हैं। लेकिन यहाँ बुनियादी मुद्दा यह है कि जनजातियों के एकीकरण ने उनकी अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की उपेक्षा की है, एकीकरण मुख्यधारा के समाज की शर्तों पर और उन्हीं को लाभान्वित करने के लिए होता रहा है। जनजातीय समाजों से उनकी ज़मीनें और वन छीन लिए गए हैं और विकास के नाम पर उनके समुदायों को छिन्न-भिन्न कर दिया गया है।
राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास
‘विकास’ की अनिवार्यताओं ने जनजातियों के प्रति राज्य के रुख या अभिवृत्तियों को शासित किया है और राज्य की नीतियों को आकार दिया है। राष्ट्रीय विकास के नाम पर, विशेष रूप से नेहरू युग में, बड़े-बड़े बाँध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और खानों की खुदाई शुरू की गई। क्योंकि जनजातीय इलाके देश के खनिज-संपन्न और वनाच्छादित भागों में स्थित थे इसलिए जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रकार के विकास से, जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्यधारा के लोग लाभान्वित हुए। खनिजों के दोहन और जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों के उपयोग, जिनमें से अनेक स्थल जनजातीय इलाकों में स्थित थे, का एक आवश्यक उप-उत्पाद यह था कि जनजातीय लोगाें से उनकी ज़मीनें छिनने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
अधिकांश जनजातीय समुदाय वनों पर आश्रित थे, इसलिए वन छिन जाने से उन्हें भारी धक्का लगा। वनों का दोहन (कटाई) तो सुव्यवस्थित रूप से ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हो गया था और वह प्रवृत्ति स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी जारी रही। ज़मीनों पर निजी मालिकाना हक (स्वामित्व) दिए जाने से भी जनजातीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि उनके यहाँ समुदाय आधारित सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी और उसके स्थान पर नयी व्यवस्था लागू किए जाने से उन्हें हानि उठानी पड़ी। इसका एक सबसे ताजा उदाहरण नर्मदा पर बनाए जा रहे बाँधों की शृंखला है जहाँ अधिकांश कीमत, अर्थात् जिन लोगों को इसकी वजह से हानि हुई है, और लाभ असंगत-अनुपात में विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को मिल रहे हैं।
जनजातीय लोगों की घनी आबादी वाले अनेक क्षेत्रों और राज्यों को विकास के दबाव के कारण गैर-जनजातीय लोगों के भारी संख्या में अप्रवास (आकर बसने) की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। इससे जनजातीय समुदायों के छिन्न-भिन्न होने और दूसरी संस्कृतियों के हावी हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। उदाहरण के लिए, झारखंड के औद्योगिक इलाकों में वहाँ की जनसंख्या में जनजातीय अनुपात कम हो गया है। लेकिन सबसे अधिक नाटकीय स्थिति संभवतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। वहाँ त्रिपुरा जैसे राज्य की जनसंख्या में जनजातीय लोगों का अनुपात एक ही दशक में घटकर आधा रह गया, जिसके परिणामस्वरूप वे अल्पसंख्यक बन गए। अरुणाचल प्रदेश में भी एेसा ही दबाव महसूस किया जा रहा है।
समकालीन जनजातीय पहचान
मुख्यधारा की प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदायों के बलात् समावेश का प्रभाव जनजातीय संस्कृति तथा
समाज पर ही नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था पर भी समान रूप से पड़ा है। आज जनजातीय पहचानें, उन जनजातियों की आदिम (मौलिक) विशिष्टताओं को जो कि सिर्फ़ जनजातियों की होती थी के बजाय, इस अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से बन रही हैं। चूँकि मुख्यधारा के साथ अंतःक्रिया आमतौर पर जनजातीय समुदायों के लिए अनुकूल शर्तों पर नहीं होती, इसलिए आज अनेक जनजातीय पहचानें गैर-जनजातीय जगत की दुर्दमनीय शक्ति का प्रतिरोध एवं विरोध करने के विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग-अलग राज्य का दर्जा मिल गया है; लेकिन एेसी सफलताओं का सकारात्मक प्रभाव पहले से चली आ रही समस्याआें के कारण तिरोहित हो गया है। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक राज्य कई दशकों से एेसे विशेष कानूनों के अंतर्गत, जिनसे वहाँ के निवासियों की नागरिक स्वतंत्रताएँ सीमित हो रही हैं, अपना जीवनयापन कर रहे हैं। इस प्रकार, मणिपुर या नागालैंड जैसे राज्यों के नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैें क्योंकि उनके राज्यों को ‘उपद्रवग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया जा चुका है। पहले सशस्त्र विद्रोह फिर उनके दमन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम और फिर उनसे भड़के विद्रोहों के दुश्चक्र ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी हानि पहुँचाई है। देश के एक अन्य भाग में झारखंड और छत्तीसगढ़ को अपने नवार्जित राज्यत्व का अभी पूरा-पूरा उपयोग करना है और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अभी तक बड़ी संरचनाओं के शिकंजे से निकलकर, जिनमें जनजातीय लोग शक्तिहीन हैं, स्वायत्त नहीं हुई हैं।
एक अन्य महत्त्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदायों में शनैः-शनैः एक शिक्षित मध्य वर्ग का उद्भव है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो यह वर्ग सर्वाधिक दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन अब यह देश के अन्य भागों में भी, विशेषकर बड़े जनजातीय समुदायों के सदस्यों में साफ़ दिखाई देने लगा है। आरक्षण की नीतियों के साथ मिलकर (जिनके बारे में आप पाँचवें अध्याय में कुछ अधिक जान सकेंगे), शिक्षा एक नगरीकृत व्यावसायिक वर्ग का निर्माण कर रही है। ज्यों-ज्यों जनजातीय समाजों में अधिकाधिक अंतर बढ़ता जाएगा अर्थात् उनके भीतर वर्गों एवं विभाजनों का विकास होता जाएगा, त्यों-त्यों जनजातीय पहचान का दावा किए जाने के लिए भिन्न-भिन्न आधार विकसित होते चले जाएँगे।
दो प्रकार के मुद्दों ने जनजातीय आंदोलनों को तूल देने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रकार के मुद्दे वे हैं जो भूमि तथा विशेष रूप से वनों जैसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से संबंधित हैं और दूसरे प्रकार के मुद्दों का संबंध नृजातीय-सांस्कृतिक पहचान के मामलों से है। यह दो मुद्दे अक्सर साथ-साथ चल सकते हैं, परंतु जनजातीय समाज में विभिन्नताएँ होने से ये अलग-अलग भी हो सकते हैं। जनजातीय समाजों में मध्यवर्गीय लोगों द्वारा अपनी जनजातीय पहचान का दावा किए जाने के कारण उन कारणों से भिन्न हो सकते हैं जिनके लिए गरीब और अशिक्षित जनजातीय लोग जनजातीय आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। जैसाकि किसी भी अन्य समुदाय के साथ होता है, इस प्रकार की अांतरिक गतिशीलताओं और बाह्य शक्तियों के बीच के संबंध ही इनके भविष्य को रूप प्रदान करेंगे।
बॉॅक्स 3.1
जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखने का आग्रह दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि जनजातीय समाज के भीतर भी एक मध्य वर्ग का प्रादुर्भाव हो चला है। विशेष रूप से इस वर्ग के प्रादुर्भाव के साथ ही, संस्कृति, परंपरा, आजीविका यहाँ तक कि भूमि तथा संसाधनों पर नियंत्रण और आधुनिकता की परियोजनाओं के लाभों में हिस्से की माँगें भी जनजातियों में अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के आग्रह का अभिन्न अंग बन गई हैं। इसलिए अब जनजातियों में उनके मध्य वर्गों से एक नई जागरूकता की लहर आ रही है। ये मध्य वर्ग स्वयं भी आधुनिक शिक्षा और आधुनिक व्यवसायाें का परिणाम है, जिन्हें सरकार की आरक्षण नीतियों से बल मिला है...
स्रोतः वर्जीनियस खाखा, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटीः द केस अॉफ ट्राइब्स इन इंडिया, जॉन 2006
3.3 परिवार और नातेदारी
हममें से हर कोई एक परिवार में उत्पन्न हुआ है और हममें से अधिकांश लोग परिवार में अनेक वर्ष बिताते हैं। आमतौर पर हम अपने परिवार से गहरा लगाव महसूस करते हैं। कभी-कभी हम अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, सहोदर भाई-बहनों, चाचा-चाचियों, मामा-मामियों तथा चचेरे-ममेरे भाइयों-बहनों के बारे में बहुत लगाव महसूस करते हैं, जबकि दूसरों के बारे में हम एेसा महसूस नहीं करते। एक ओर तो हम उनके हस्तक्षेप के लिए अप्रसन्नता या रोष प्रकट करते हैं, फिर भी जब हम उनसे दूर रहते हैं तो उनके रोबदाबपूर्ण तरीकों के लिए तरसते हैं और उन्हें याद करते हैं। परिवार गहरे स्नेह एवं देखभाल का स्थान है। दूसरी ओर, यह कटु संघर्षों, अन्याय और हिंसा का स्थान भी हो सकता है। परिवार और नातेदारी में मादा शिशु की हत्या, संपत्ति के लिए भाइयों के बीच हिंसापूर्ण लड़ाई-झगड़े और घिनौने कानूनी विवाद भी इसका वैसे ही एक हिस्सा होते हैं जैसे प्यार, त्याग एवं बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा एवं देखभाल की कहानियाँ हैं।
परिवार की संरचना का अध्ययन इसके एक सामाजिक संस्था के रूप में और समाज की अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ उसके संबंधों के बारे में, दोनों ही रूप में किया जा सकता है। स्वयं परिवार को मूल परिवार अथवा विस्तृत परिवार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका मुखिया (कर्ता) एक पुरुष या स्त्री भी हो सकती है। वंशानुक्रम की दृष्टि से परिवार मातृवंशीय अथवा पितृवंशीय हो सकता है। परिवार की यह आंतरिक संरचना आमतौर पर, समाज की अन्य संरचनाओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि संरचनाओं से जुड़ी होती है। इस प्रकार, हिमालयी क्षेत्र के गाँवों से पुरुषों के प्रवसन से उस गाँव में एेसे परिवारों का अनुपात असामान्य रूप से बढ़ सकता है जिनकी मुखिया स्त्रियाँ हैं। या भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्य कर रहे युवा माता-पिता का कार्य-समय एेसा हो कि वे अपने बच्चों की देखभाल ठीक से न कर सकें तो वहाँ दादा-दादियों तथा नाना-नानियों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि उन्हें ही वहाँ आकर बच्चों की देखभाल करनी होगी। इस प्रकार, परिवार की संरचना अथवा उसके गठन में परिवर्तन हो जाता है। और इन परिवर्तनों को समाज में होने वाले अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में समझा जा सकता है। परिवार (निजी क्षेत्र) आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृृतिक, शैक्षिक (सार्वजनिक) क्षेत्रों से जुड़ा होता है।
बॉॅक्स 3.2
प्रस्तुत अध्ययन...मुलतानी लोहार कही जाने वाली एक मुस्लिम बिरादरी से संबंधित है।... कारखानेदार एक देशी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग एक एेसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो एेसे निर्माण व्यवसाय में संलग्न हो जिसका आमतौर पर वह खुद मालिक हो ... कारखाने, जिनका अध्ययन किया गया है, घरेलू परिस्थितियों में चलाए जाते हैं और इसलिए उनका उन कारखानेदारों की ज़िंदगी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जो उन कारखानों में काम करते हैं।... निम्नलिखित मामला इस स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
महमूद, उम्र चालीस साल, अपने दो छोटे भाइयों के साथ रहता था, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी। महमूद के तीन बच्चे थे और वह उस मिश्रित परिवार का मुखिया था। ... तीनों भाई विभिन्न कारखानों और फैक्ट्रियों में कुशल कामगार के रूप में काम करते थे। महमूद एक एेसे मोटर पुर्जे की प्रतिकृति (नकली पुर्जा) बनाने में सफल हो गया जिसका आयात प्रतिबंधित था। अपनी इस सफलता से प्रोत्साहित होकर उसने अपना खुद का कारखाना चालू कर दिया ... आगे चलकर, यह फ़ैसला किया गया कि उस मोटर पार्ट को बनाने के लिए दो कारखाने लगाए जाएँ। इनमें से एक कारखाने के मालिक दोनों बड़े भाई हों और सबसे छोटे भाई को दूसरे कारखाने का मालिक बना दिया जाए, बशर्ते कि वह अपना अलग घर बसा ले। रशीद ने अपनी पत्नी और अविवाहित बच्चों को लेकर स्वतंत्र रूप से अपना अलग घर बसा लिया। इस प्रकार, एक मिश्रित परिवार ने, जिसमें तीन शादीशुदा भाई थे, एक साधारण छोटे से परिवार को पैदा कर दिया। यह नया छोटा परिवार नए उद्यमी अवसरों की देन था।
स्रोतः एस.एम. अकरम रिजवी के ‘किनशिप एंड इंडस्ट्री अमंग द मुस्लिम कारखानेदार्स इन देहली’, इमतियाज अहमद द्वारा संपा. फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया’ 1976, मनोहर, पृ. 27-48 नई दिल्ली से उद्धृत
परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे लिए इसका अस्तित्व स्वतः स्वीकृत है। हम यह भी मानकर चलते हैं कि अन्य लोगों के परिवार भी हमारे परिवार की तरह ही होंगे। (परिवार के इस आयाम और अन्य आयामों पर भी ग्यारहवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक ‘समाजशास्त्र परिचय’ के तीसरे अध्याय में चर्चा की जा चुकी है)। तथापि हमने देखा है कि परिवारों की संरचनाएँ भिन्न-भिन्न होती है और यह बदलती भी रहती हैं। यह परिवर्तन कभी-कभी तो आकस्मिक तौर पर होते रहते हैं जब कोई लड़ाई छिड़ जाती है अथवा लोग काम की तलाश में अन्यत्र जा बसते हैं। कभी-कभी यह परिवर्तन किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, जैसे कि जब युवा लोग बुज़ुर्गों द्वारा उनके लिए जीवन-साथी का चुनाव करने के बजाय स्वयं ही अपने जीवन-साथी का चुनाव कर लेते हैं। अथवा जब समाज में समलैंगिक प्यार का खुले तौर पर इजहार किया जाता है।
उपर्युक्त प्रकार के परिवर्तनों से यह स्पष्ट है कि परिवार की संरचनाओं में ही बदलाव नहीं आता बल्कि सांस्कृतिक विचार, मानकों और मूल्यों में भी परिवर्तन होते हैं। किंतु, इस प्रकार के परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। इतिहास और आधुनिक काल की घटनाओं से पता चलता है कि अक्सर पारिवारिक और वैवाहिक प्रतिमानों में किए जाने वाले परिवर्तनों का घोर हिंसात्मक विरोध किया जाता है। इस संबंध में परिवार के भी कई आयाम होते हैं। किंतु भारत में, परिवार विषयक चर्चाएँ अक्सर मूल और विस्तृत परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं।
मूल एवं विस्तारित परिवार
मूल परिवार में माता-पिता (दंपति) और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। विस्तृत परिवार (जिसे आमतौर पर ‘संयुक्त परिवार’ कहा जाता है) के भिन्न-भिन्न रूप हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक से अधिक युगल (दंपति) होते हैं और अक्सर दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एकसाथ रहते हैं। इसमें कई भाई भी हो सकते हैं जो अपने-अपने परिवारों को लेकर संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं या एक बुज़ुर्ग दंपति जो अपने बेेटों, पोतों, उनके परिवारों के साथ रहते हों। विस्तृत परिवार अक्सर भारतीय होने का सूचक माना जाता है। लेकिन अब, बल्कि पहले भी यह किसी भी अर्थ में परिवार का प्रमुख रूप नहीं रहा है। यह समुदाय के कुछ अनुभागों या कतिपय क्षेत्रों तक ही सीमित था। वास्तव में, अंग्रेज़ी का ‘ज्वाइंट फैमिली’ (Joint family) शब्द ही, जिसे हिंदी में ‘संयुक्त परिवार’ कहा जाता है, देशज नहीं है। जैसाकि आई. पी. देसाई ने कहा है, "अंग्रेज़ी का ‘ज्वाइंट फैमिली’ शब्द किसी भी एेसे भारतीय शब्द का अनुवाद नहीं है। यह बात रुचिकर है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में संयुक्त परिवार के लिए प्रयुक्त शब्द अंग्रेज़ी भाषा के ‘ज्वाइंट फैमिली’ शब्द का ही अनुवादित पर्याय है" (देसाई 1964:40)।
परिवार के विविध रूप
अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न समाजों में किस तरह विविध प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले में पत्नी-स्थानिक और कुछ पति-स्थानिक होते हैं। पहली स्थिति में नवविवाहित जोड़ा वधू के माता-पिता के साथ रहता है और दूसरी स्थिति में, वर के माता-पिता के साथ। उत्तराधिकार के नियम के अनुसार, मातृवंशीय समाज में जायदाद माँ से बेटी को मिलती है और पितृवंशीय समाज में पिता से पुत्र को। पितृतंत्रात्मक परिवार संरचना में पुरुषों की सत्ता व प्रभुत्व होता है और मातृतंत्रात्मक परिवार संरचना में स्त्रियाँ समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। हालाँकि पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक कल्पना है। मातृतंत्र का कोई एेतिहासिक या मानवशास्त्रीय प्रमाण नहीं है अर्थात् एेसा समाज नहीं है जहाँ स्त्रियाँ प्रभुत्वशाली हों। हालाँकि मातृवंशीय समाज अवश्य पाए जाते हैं अर्थात् एेसे समाज जहाँ स्त्रियाँ अपनी माताओं से उत्तराधिकार के रूप में जायदाद पाती हैं परंतु उस पर उनका अधिकार नहीं होता और न ही सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार होता है।
बॉक्स 3.3 में दिया खासी मातृवंश का विवरण मातृवंश और मातृतंत्र के बीच के अंतर को स्पष्ट करेगा। यह विवरण मातृवंश द्वारा उत्पन्न उन संरचनात्मक तनावों के बारे में भी बतायेगा जिससे समकालीन खासी समाज के पुरुष और स्त्रियाँ प्रभावित होते हैं।

बॉॅक्स 3.3
मेघालय उत्तराधिकार अधिनियम (मेघालय विधानसभा, जिसके सभी सदस्य पुरुष ही थे, द्वारा पारित) को 1986 में राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली। अधिनियम विशेष तौर पर खासी और जैन्तिया जनजाति पर लागूू होता है और ‘उस खासी या जैन्तिया व्यक्ति पर मान्य है जो बुद्धि से सबल है और अल्पआयु नहीं है; उस व्यक्ति को अपनी खुद की बनाई हुए जायदाद की वसीयत बनाने का अधिकार है’।
वसीयत बनाने की प्रथा, खासियों में नहीं है। खासी प्रथा मातृ वंशज के आधार पर जायदाद को अमुक स्त्री को सुपुर्द किए जाने की बात करती है।
खासियों में, विशेषतः पढ़े-लिखे खासियों को एेसा प्रतीत होता है कि उनके संबंधों और उत्तराधिकार के नियम, स्त्रियों के पक्ष में हैं और अपने आप में सीमित भी हैं। अतः यह अधिनियम खासी परंपरा में व्याप्त महिलाओं के पक्ष में किए गए पक्षपात को ठीक कर इस सीमितता को समाप्त करने का एक प्रयास है। यह परखने के लिए कि क्या ये प्रचलित बोधता–जो खासी परंपरा में स्त्रियों के प्रति पक्षपात की बात करती है, सही है कि नहीं, यह ज़रूरी है कि खासी मातृवंशीय व्यवस्था को व्यावहारिक लिंग-संबंधों और लिंग भूमिकाओं की परिभाषाओं के संदर्भ में देखा जाए।
कई विशेषज्ञों ने मातृवंशीय व्यवस्थाओं में अंतर्निहित विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित किया है। एक एेसा विरोधाभास वंशानुक्रम की रेखा और उत्तराधिकार एवं नियंत्रण और सत्ता की संरचना के अलगाव से उत्पन्न होता है। पहला संदर्भ जो माँ और बेटी को जोड़ता है वह दूसरे संदर्भ के आ जाने से प्रतिद्वंद्विता की उत्पत्ति होती है जो माँ के भाई को बहन के बेटे से जोड़ता हैै [दूसरे शब्दों में, एक स्त्री अपने माँ से जायदाद उत्तराधिकार में पाती है और आगे अपनी बेटी को देती है, जबकि एक पुरुष अपनी बहन की जायदाद पर नियंत्रण रखता है, और वो नियंत्रण अपनी बहन के बेटे को देता है। इस तरह संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकार तो माँ से बेटी को जाता है पर व्यावहारिक रूप में यह अधिकार मामा से भानजे को जाता है]।
खासी मातृवंश पुरुषों के लिए गहन भूमिका द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों एवं जन्म के घर की ज़िम्मेदारियों के बीच बँट जाते हैं। एक तरह से भूमिका-द्वंद्व द्वारा उत्पन्न इस तनाव का असर खासी स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक स्त्री कभी सुनिश्चित नहीं कर सकती कि उसके पति को उसकी बहन का घर ज़्यादा अच्छा लगता है या अपना स्वयं का। उसी तरह बहन सोचेगी कि शादीशुदा भाई अपनी बहन के प्रति ज़िम्मेदारियों को भूल जाएगा।
खासी मातृवंशीय व्यवस्था में उत्पन्न भूमिका-द्वंद्व से पुरुषों की बजाय अंततः स्त्रियाँ ज़्यादा गहन रूप से प्रभावित होती हैं, सिर्फ़ इसलिए नहीं क्योंकि पुरुष अधिकारों के स्वामी हैं और स्त्रियाँ इससे वंचित हैं पर इसलिए भी क्योंकि समाज पुरुषों को नियम तोड़ने पर उन्हें कम सज़ा देता है या नज़र अंदाज़ कर देता है। खासी समाज में स्त्रियों के पास सिर्फ़ नाम का अधिकार होता है–असली अधिकार पुरुषों के हाथ में होता है। हाँ, इतना ज़रुर है कि यह व्यवस्था पुरुष के मातृ-नातेदार की तरफ़ झुकी हुई है न कि पितृ-नातेदार की तरफ़। (दूसरे शब्दों में मातृवंश के बावजूद, पुरुष ही खासी समाज में शक्ति के स्वामी हैं; सिर्फ़ एक अंतर है कि एक पुरुष के लिए उसकी माँ की तरफ़ के रिश्तेदारों का उसके पिता की तरफ़ के रिश्तेदारों से ज़्यादा महत्त्व होता है)।
स्रोतः तिपलुत नोंगब्री के लेख ‘जेन्डर एंड द खासी फैमिली स्ट्रक्चर’, ओबरॉय द्वारा संपा. 1994 से उद्धृत
प्रश्नावली
1. जाति व्यवस्था में पृृथक्करण (separation) और अधिक्रम (hierachy) की क्या भूमिका है?
2. वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है? कुछ के बारे में बताइए?
3. उपनिवेशववाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या-क्या परिवर्तन आए?
4. किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत ‘अदृश्य’ हो गई है?
5. भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है?
6. ‘जनजातियाँ आदिम समुदाय हैं जो सभ्यता से अछूते रहकर अपना अलग-थलग जीवन व्यतीत करते हैं’, इस दृष्टिकोण के विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे?
7. आज जनजातीय पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण हैं?
8. परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं?
9. सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं?
10. मातृवंश (matriliny) और मातृतंत्र (matriarachy) में क्या अंतर है? व्याख्या कीजिए।
संदर्भ ग्रंथ
देशपांडे, सतीश. 2003. कंटम्प्रेरी इंडियाः ए सोसियोलॉजीकल व्यू. पैंगुइन बुक्स. नयी दिल्ली।
गुप्ता, दीपांकर. 2000. इंटेरोगेटिंग कास्ट. पैंगुइन बुक्स. नयी दिल्ली।
शर्मा, के. एल. संपा. 1999. सोशल इनइक्वालिटी इन इंडियाः प्रोफिट्स अॉफ कास्ट, क्लास एंड सोशल मोबिलिटी. द्वितीय संस्करण. रावत पब्लिकेशंस. जयपुर।
शर्मा, उर्सुला. 1999. कास्ट. ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस. बकिंघम एंड फिलाडेल्फिया।
बेते, आंद्रे. 1991. ‘द रिप्रोडक्शन अॉफ इनइक्वालिटीः अॉक्यूपेशन, कास्ट एंड फैमिली’, कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन सोसियोलॉजी. से एन. एस., वॉल्यूम. 25, नं. 1, पृष्ठ संख्या 3-28।
श्रीनिवास, एम. एन. 1994. द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एस्सेज. अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. नयी दिल्ली।
डयूमो, लूई. 1981. होमो हेरारकिकसः द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इंप्लीकेशंस. द्वितीय संस्करण. यूनिवर्सिटी अॉफ शिकागो प्रेस. शिकागो।
घुरिये, जी. एस. 1969. कास्ट एंड रेस इन इंडिया. पाँचवाँ संस्करण, पॉपुलर प्रकाशन. मुंबई।
जॉन, मैरी ई. प्रवीन, कुमार झा. एवं सुरिन्दर, एस. जोधका. संपा. 2006. कंटेस्टेड ट्रांसफॉरमेशंसः चेंजिंग इकोनॉमीज एंड आइडेंटिटीस इन कंटम्प्रेरी इंडिया. तूलिका. नयी दिल्ली।
डिर्क, निकलस. 2001. कास्ट्स अॉफ माइंडः कोलोनियलिज़्म एंड द मेकिंग अॉफ मॉडर्न इंडिया. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस. प्रिंसटन।
ओबेरॉय, पेट्रीशिया. संपा. 1994. फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया. अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. दिल्ली।
वर्जीनियस, खाखा. 2003. ‘ट्राइब्स इन इंडिया’ वीना, दास. द्वारा संपा. द अॉक्सफोर्ड इंडिया कंपेनियन टू सोसियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपॉलोजी. अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. दिल्ली।